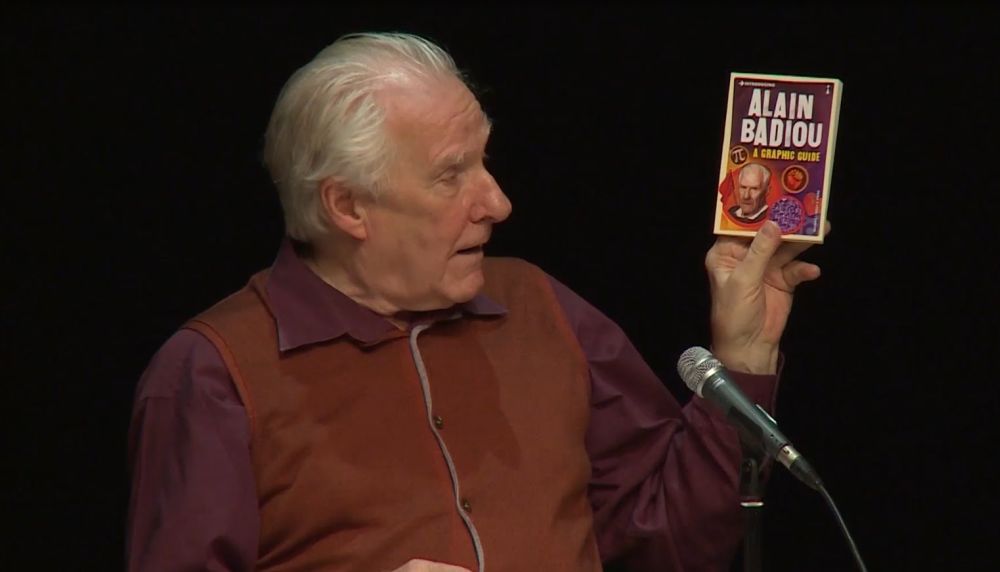उत्तर-मार्क्सवाद के ‘कम्युनिज़्म’ : उग्रपरिवर्तन के नाम पर परिवर्तन की हर परियोजना को तिलांजलि देने की सैद्धान्तिकी
- शिवानी, बेबी
विचार
जब सिर्फ़ विचार होते हैं
अस्पष्ट होते हैं
प्रशंसनीय होते हैं।
विचार जब
व्यापकता पाते हैं
योजनाओं में ढलते हैं
योजनाएँ जब
गतिशील होती हैं
आपत्तियाँ सिर उठाती हैं।
– बेर्टोल्ट ब्रेष्ट
दार्शनिकों ने
दुनिया की तरह-तरह से व्याख्या की है
पर सवाल उसको बदलने का है,
मानता हूँ।
लेकिन फि़लहाल मैं असन्तुष्ट हूँ
दुनिया की व्याख्याओं से
और मानता हूँ कि
नये बदलावों की हो रही व्याख्याएँ
या तो नाकाफ़ी या फिर ग़लत हैं
और यह कि
रुका हुआ है आज
दुनिया को बदलने का काम भी।
इसलिए अभी तो मैं
दुनिया की एक और व्याख्या कर रहा हूँ।
– कात्यायनी (दुनिया को बदलने के बारे में कतिपय सुधीजनों के विविध विचार-1)
”उत्तर-मार्क्सवाद के ‘कम्युनिज़्म’” – इस विषय पर एक आलेख की ज़रूरत क्यों? क्या मार्क्सवाद का दौर बीत चुका है और कोई उत्तर-मार्क्सवादी दौर शुरू हो गया है? इस आलेख के आरम्भ में ही हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे विचार में एक विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद के सामने कोई संकट नहीं है लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मार्क्सवाद पर विचारधारात्मक हमलों का सिलसिला आज तक बदस्तूर जारी है। फ़र्क़ बस इतना है कि 1989 में बर्लिन की दीवार के गिरने और 1990 में सोवियत संघ के औपचारिक विघटन के साथ विचारधारा और राजनीति की दुनिया में पूँजीवादी विजयवाद की उन्मत्त घोषणाओं की तरह ये नये बौद्धिक आक्रमण उतने खुले और आवरणहीन नहीं हैं। आज के दौर में, एक बार फिर, बुर्जुआ सांस्कृतिक और बौद्धिक उपकरण मार्क्सवाद पर नये हमले कर रहे हैं और कम्युनिस्ट आन्दोलन से लेकर छात्रों, बुद्धिजीवियों आदि के बीच विभ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी अनायास नहीं है कि पूँजीवाद, अपने वर्चस्वकारी मैकेनिज़्म के ज़रिये सहज गति से तमाम कि़स्म के रंग-बिरंगे ‘रैडिकल’ बुद्धिजीवियों को पैदा कर रहा है, जो मार्क्सवाद की बुनियादी प्रस्थापनाओं पर चोट कर रहे हैं। उत्तर-मार्क्सवादियों की एक पूरी धारा है जो उग्र-परिवर्तनवादी जुमलों का सहारा लेकर मार्क्सवाद की क्रान्तिकारी अर्न्तवस्तु पर निशाना साध रही है। ऐलन बेदियू, स्लावोय ज़िज़ेक, एण्टोनियो नेग्री, माइकल हार्ट, ज़ाक रैंसिये, अर्नेस्टो लाक्लाऊ, चैण्टेल माउफ़ आदि जैसे तमाम ”रैडिकल दार्शनिक” इसी उत्तर-मार्क्सवादी विचार-सरणि से आते हैं। एक बात जिसे यहाँ पर विशेष तौर पर रेखांकित करने की ज़रूरत है वह यह कि मार्क्सवाद पर जो भी विचारधारात्मक-बौद्धिक हमले होते रहे हैं या फिर हो रहे हैं, उनके नाम नये हो सकते हैं लेकिन उनकी अन्तर्वस्तु में कुछ भी नया नहीं है, जैसा कि एक बार एक अलग सन्दर्भ में ज्याँ पॉल सार्त्र ने कहा था। सार्त्र ने कहा था कि मार्क्सवाद-विरोधी विचारधाराएँ जो कुछ सही कह रही हैं, वह मार्क्सवाद पहले ही कह चुका है और जो कुछ वे नया कह रही हैं वह ग़लत है! उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर-संरचनावाद, प्राच्यवाद, उत्तर-प्राच्यवाद, सबऑल्टर्निज़्म जैसी तमाम ‘उत्तर-’ विचार-सरणियों की ”चुनौतियों” का क्या हश्र हुआ, यह हम सभी जानते हैं। ये सभी विचार-सरणियाँ विचारधारात्मक कोमा में पड़ी आख़िरी साँसें गिन रही हैं! उत्तर-मार्क्सवादी दर्शन और सिद्धान्त इन्हीं कि़स्म-कि़स्म की ‘उत्तर-’ विचार सरणियों का एक ‘अपग्रेडेड वर्जन’ है।
हालाँकि मार्क्सवाद पहले ही ऐसे तमाम विचारधारात्मक और सैद्धान्तिक हमलों का जवाब दे चुका है; लेकिन आज जो नये विचारधारात्मक हमले हैं, वे कम से कम ऊपर से पूँजीवाद की अन्तिम विजय की बात नहीं कर रहे हैं। उल्टा वे पूँजीवाद से आगे जाने और कई बार ‘कम्युनिज़्म’ की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उनके ‘कम्युनिज़्म’ के विस्तार में जाते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें नाम के अतिरिक्त कुछ भी कम्युनिस्ट नहीं है! वे मार्क्सवाद से ज़्यादा ‘रैडिकल’ किसी विचारधारा की माँग रख रहे हैं, मार्क्सवाद से आगे जाने का दावा कर रहे हैं, और मार्क्स की शिक्षाओं की प्रासंगिकता समाप्त होने का दावा कर रहे हैं; उनका दावा है कि हम मार्क्सवादी कम्युनिज़्म से आगे आ चुके हैं और अब उत्तर-मार्क्सवादी कम्युनिज़्म का दौर है! आगे हम इनके उत्तरमार्क्सवादी ‘कम्युनिज़्मों’ की अन्तर्वस्तु की विस्तार से पड़ताल करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि एक बार फिर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन का एक अहम कार्यभार यह भी बन जाता है कि ऐसे विचारधारात्मक हमलों के बरक्स न सिर्फ़ मार्क्सवाद की दृढ़ता से हिफ़ाजत की जाये बल्कि इन हमलों का मुँहतोड़ जवाब भी दिया जाये और दिखलाया जाये कि इन ‘नये’ हमलों में कुछ भी नया नहीं है और दरअसल पुराने बुर्जुआ सिद्धान्तों की ‘शराब’ को ही नयी फ़ैशनेबुल फ़्रांसीसी दर्शन की ‘बोतल’ में परोस दिया गया है। विशेषकर उत्तर-मार्क्सवादी चिन्तन पर कठोरता से चोट किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस चिन्तन सरणि के अधिकांश रैडिकल ‘दार्शनिक’ एक नये कि़स्म के ‘कम्युनिज़्म’ की बात कर रहे हैं। क्रान्तिकारी छात्रों-युवाओं और बुद्धिजीवियों का भी एक अच्छा-ख़ासा हिस्सा इन उत्तर-मार्क्सवादी चिन्तकों के ”चिन्तनों” के प्रभाव में आकर इनके मार्क्सवाद-विरोधी विजातीय विचारों को ही मार्क्सवाद और कम्युनिज़्म का सिद्धान्त मानने की भूल कर रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए, स्लावोय ज़िज़ेक और ऐलन बेदियू जैसे उत्तर-मार्क्सवादी सिद्धान्तकार लेनिन और माओ की संकलित रचनाओं का सम्पादन करते हुए जो प्रस्तावनाएँ और परिशिष्ट लिख रहे हैं, उनमें वे कौन से विचार व्यक्त कर रहे हैं? ये दोनों ही और इनके अलावा अन्य उत्तर-मार्क्सवादी चिन्तक भी, लेनिन, माओ और साथ ही मार्क्स का भी, अपने उत्तर-मार्क्सवादी दर्शन के अनुरूप हस्तगतीकरण (ंappropriation) करते हैं और वस्तुतः मार्क्सवाद की क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तु पर चोट करते हैं। इस तरह ये सभी ‘रैडिकल विचारक’ क्रान्ति के भर्ती केन्द्रों और भावी पाँतों में विभ्रम और विचारधारात्मक प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन्हें माक़ूल जवाब देना आज का एक ज़रूरी कार्यभार है। साथ ही इस उत्तर-मार्क्सवादी दर्शन के ग़ैर-मार्क्सवादी सैद्धान्तिकीकरणों का प्रभाव भारत समेत दुनिया भर के वामपन्थी दायरे के कुछ हिस्सों पर भी है, परिणामस्वरूप जिसका ‘रिपल इफ़ेक्ट’ अन्य स्थानों (कॉलेज, विश्वविद्यालय, बौद्धिक-सांस्कृतिक प्रतिष्ठान) पर देखा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो उत्तर-मार्क्सवादी दर्शन और सिद्धान्त की एक प्रबल मार्क्सवादी आलोचना आज के दौर का एक महत्वपूर्ण विचारधारात्मक कार्यभार बन जाता है। यह आलेख इसी दिशा में एक प्रयत्न है।
उत्तर-मार्क्सवादी सैद्धान्तिकी की विस्तृत और वृहत् समालोचना में जाने से पहले हम यहाँ कुछेक बातें साझा कर लेना चाहते हैं। हम अपने आलेख में विभिन्न उत्तर-मार्क्सवादी सिद्धान्तकारों के राजनीतिक दर्शन से जुड़े सैद्धान्तिकीकरणों की पड़ताल करेंगे। विशेष तौर पर यह आलेख इस पर केन्द्रित होगा कि बीसवीं सदी के समाजवादी प्रयोगों (ख़ास तौर पर रूस और चीन में हुए प्रयोगों), समाजवादी संक्रमण और कम्युनिज़्म के विषय में उत्तर-मार्क्सवादी अवस्थिति क्या है; साथ ही, भविष्य की राजनीति/मुक्तिकामी राजनीति (Emancipatory politics) पर तमाम उत्तर-मार्क्सवादी दार्शनिकों के क्या विचार हैं, हम इसकी भी पड़ताल करेंगे। इसके अलावा उत्तर-मार्क्सवाद के प्रमुख दार्शनिक राजनीतिक स्रोतों और प्रभावों की भी चर्चा हम करेंगे। एक बात जिसे हम यहाँ पर ज़ोर देकर रेखांकित करना चाहते हैं वह यह कि उत्तर-मार्क्सवादी चिन्तन की एक सम्पूर्ण दार्शनिक समालोचना इस आलेख की विषय-वस्तु नहीं है। राजनीतिक-विचारधारात्मक मुद्दों पर इस चिन्तन-सरणि की आलोचना के लिए जहाँ हमें उसके दार्शनिक मूलों पर जाना पड़ा, केवल वहीं हम उसके दर्शन का जि़क्र करेंगे। वैसे राजनीतिक-विचारधारात्मक समालोचना अपने आप में उत्तर-मार्क्सवाद के दर्शन के बारे में भी काफ़ी कुछ बताती है।
उत्तर-मार्क्सवादी सैद्धान्तिकी का इतिहास-भूगोल एवं मुख्य
दार्शनिक-राजनीतिक स्रोत
जिसे आमतौर पर उत्तर-मार्क्सवाद की संज्ञा दी जाती है, वह अपने आप में कोई एकाशमी (monolithic) या सजातीय (homogeneous) चिन्तन-प्रणाली नहीं है। कई मुद्दों पर इस विचार-सरणि के तहत आने वाले सिद्धान्तकार एक-दूसरे की बातों को काटते हुए भी नज़र आते हैं। हालाँकि तमाम भिन्नताओं और वैषम्य के बावजूद मार्क्सवाद की मूल क्रान्तिकारी प्रस्थापनाओं के खण्डन और बीसवीं सदी के समाजवादी प्रयोगों के नकारात्मक आकलन के विषय में यह सभी सिद्धान्तकार एक मत हैं। इनमें से अधिकांश जिस नये कम्युनिज़्म की बात करते हैं, वह मार्क्सवादी नहीं होगा! बीसवीं सदी के मार्क्सवादी कम्युनिज़्म का अन्त एक विपदा/दुर्गति में हुआ, इसलिए एक नये कि़स्म के कम्युनिज़्म की ज़रूरत है! आज के दौर में पार्टी और राज्य जैसी अवधारणाएँ अप्रासंगिक हो चुकी हैं (श्रीमान बेदियू)! पूँजीपति वर्ग के बजाय ये दमनकारी ‘शासक’ (rulers) और सर्वहारा वर्ग की जगह ‘बहुसंख्या’ (multitude) शब्द का इस्तेमाल बहुत पसन्द और चाव के साथ करते हैं; पूँजी, उत्पादन, सम्पत्ति आदि जैसी श्रेणियों की जगह ये साझा (commons) की बात करना पसन्द करते हैं (श्रीमान नेग्री व श्रीमान हार्ट तथा श्रीमान ज़िज़ेक भी)! कुछ ऐसे हैं जो मार्क्सवादी कम्युनिज़्म के आगे जाने का भी दावा नहीं करते, और उसे मानने का भी दावा नहीं करते, न ही वे राज्य और पार्टी की ज़रूरत के बारे में कुछ साफ़ कहते हैं; सर्वहारा अधिनायकत्व के बारे में भी हर वर्ष वे नियम से अवस्थिति बदलते हैं; लेकिन इतना वे ज़रूर कहते हैं कि बीसवीं सदी के समाजवादी प्रयोग एक ‘आपदा’ के रूप में ख़त्म हुए और इसलिए आज के कम्युनिज़्म का ‘विचार’ उससे सर्वथा भिन्न होगा और नारा देते हैं कि ‘बीसवीं सदी बीत गयी!’ (श्रीमान् ज़िज़ेक)! कुछ इन सब बातों में यह जोड़ देते हैं कि सर्वहारा वर्ग/दमित वर्ग/अधीनस्थ वर्ग को किसी नेतृत्व या हिरावल की आवश्यकता नहीं है; वे दमित की ”स्वशिक्षा” के पक्षधर हैं और कहते हैं आज की ज़रूरत मार्क्सवाद से ज़्यादा रैडिकल सोच की है, क्योंकि मार्क्सवाद स्वयं सत्तावादी, दमनकारी और अपचयनवादी है (श्रीमान रैंसिये)! इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हर प्रकार की सार्वभौमिकता (universality) का नाश करने की ठान रखी है और कह रहे हैं कि सार्वभौमिकता, निरपेक्षता, सामान्यता की सभी बातें वास्तव में दमनकारी होती हैं; इसलिए हमें खण्डों की हिफ़ाज़त में तन-मन-धन से लग जाना चाहिए, यानी कि, वर्ग जैसी अवधारणाएँ, सर्वहारा वर्ग की एकता जैसी अवधारणाएँ ही दमनकारी हैं और हमें टुकड़ों का जश्न मनाना चाहिए (सुश्री जुडिथ बटलर, श्रीमान लाक्लाऊ व सुश्री माउफ़)।
इन तमाम ”मौलिक” प्रस्थापनाओं के बाद ऐसे सभी ”दार्शनिकों” को सट्टेबाज़ (speculative) और बहेतू (vagabond) दार्शनिक ही कहा जा सकता है क्योंकि इनके ”चिन्तन” की कोई धुरी नहीं है। आप अगर ग़ौर करें तो पायेंगे कि तमाम रैडिकल तेवर, उग्रपरिवर्तनवादी जुमलों और नये कि़स्म की मुक्तिकामी राजनीति का पक्ष रखने के दावों के बावजूद इनका निशाना ठीक वे अवधारणाएँ हैं जो मार्क्सवाद की क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तु का निर्माण करती हैं। मिसाल के तौर पर वर्ग की अवधारणा, सर्वहारा अधिनायकत्व की अवधारणा, वर्ग के हिरावल के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी की अवधारणा, पूँजी की अवधारणा, अलगाव और शोषण की अवधारणा, आदि। ये तमाम उत्तर-मार्क्सवादी ”स्पेक्युलेटिव दार्शनिक” या तो इन अवधारणाओं को नकार देते हैं या उन्हें विकृत कर देते हैं। इनकी छद्म दार्शनिक जालसाज़ियों (जो कि आम तौर पर फै़शनेबल उत्तर-आधुनिकतावादी, फ़्रांसीसी दार्शनिक शब्दावली के आवरण में परोसी जाती हैं) को समझना हो तो इनका दार्शनिक और राजनीतिक स्रोत देखना होगा। वास्तव में, इनमें से अधिकांश का स्रोत वही है जो कि उत्तर-आधुनिकतावादी विचार सरणियों का था – यानी, मई 1968 का छात्र-मज़दूर आन्दोलन जिसका केन्द्र पेरिस था। सोवियत साम्राज्यवाद के पूर्वी यूरोप में किये गये हस्तक्षेप और पूर्वी यूरोप के छद्म समाजवादी देशों में जनता का अनुभव 1960 के दशक में सोवियत साम्राज्यवाद के प्रति आक्रोश का कारण बना। यूरोप में और विशेषकर फ़्रांस में तमाम ऐसे राजनीतिक और दार्शनिक चिन्तक थे, जिनकी विचारधारात्मक शुरुआत एक मार्क्सवादी के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में सोवियत साम्राज्यवाद के अनुभव के कारण उनका मोहभंग मार्क्सवाद से ही हो गया क्योंकि वे क्रान्तिकारी मार्क्सवाद और संशोधनवाद, समाजवाद और सामाजिक-साम्राज्यवाद के बीच फ़र्क़ नहीं देख पाये। बेदियू, ज़िजे़क, नेग्री जैसे तमाम उत्तर-मार्क्सवादियों की वर्तमान राजनीतिक अवस्थिति के मूल को यूरोपीय वाम की, यूरोपीय, विशेषकर फ़्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी के संशोधनवाद और सोवियत संघ के सामाजिक फ़ासीवाद और सामाजिक साम्राज्यवाद के कुकृत्यों से पैदा हुए राजनीतिक ‘ट्रामा’ में देखा जा सकता है। यूरोपीय देशों की कम्युनिस्ट पार्टियाँ, मिसाल के तौर पर फ़्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी (पी.सी.एफ़.), इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी (पी.सी.आई.) आदि 1960 के दशक से ही संशोधनवाद का रास्ता पकड़ चुकी थीं। 1953 में सोवियत संघ में ख्रुश्चेवी संशोधनवाद आने के बाद भी ये तमाम पार्टियाँ उसका समर्थन कर रही थीं और हंगरी, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया जैसे पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत साम्राज्यवाद के कुकृत्यों को लेकर या तो चुप थीं या समझौतापरस्त अवस्थिति अपना रही थीं। ऐसे में, इन संशोधनवादी सामाजिक-जनवादी पार्टियों से मोहभंग हो जाना लाजि़मी था। लेकिन मई 1968 में यूरोपीय वाम और यूरोपीय रैडिकल बुद्धिजीवी वर्ग ने सोवियत संशोधनवाद और उसके कुकर्मों और यूरोपीय सामाजिक-जनवादी पार्टियों के सुधारवाद और बुर्जुआ सत्ता से प्रणय पर जो प्रतिक्रिया दी, वह एक रोगात्मक प्रतिक्रिया (pathological reaction) थी, क्योंकि उसमें कोई आलोचनात्मक विवेक नहीं था। सोवियत संशोधनवादी पार्टी और सामाजिक साम्राज्यवादी व सामाजिक फ़ासीवादी राज्य के अपराधों को मार्क्सवाद की पार्टी, राज्य और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की अवधारणा पर ही आरोपित कर दिया गया। बेदियू, ज़िज़ेक जैसे तमाम उत्तर-मार्क्सवादी चिन्तक इसी पैथोलॉजिकल प्रतिक्रिया का अंग थे। साथ ही, उसी समय चीन में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति भी जारी थी, जिसे बहुतों ने ‘पार्टी के विरुद्ध क्रान्ति’ समझा (स्वयं बेदियू भी इसी समझदारी से ग्रस्त हैं।) कुल मिलाकर, नतीजा यह हुआ कि ये तथाकथित ‘नव दार्शनिक’ (New Philosophers) सारी बुराई की जड़ पार्टी और सर्वहारा अधिनायकत्व के सिद्धान्त को समझने लगे। इनमें से कुछ मार्क्सवाद को सर्वसत्तावादी, दमनकारी आदि कहते हुए उत्तर-आधुनिकतावाद की ओर चले गये, जैसे कि मिशेल फूको, ज़ाक देरीदा, आदि। और कुछ ऐसे थे जो नये कि़स्म के मार्क्सवाद की बात करने लगे! इनमें से कुछ अल्थूसर के छात्र थे। ऐलन बेदियू, ज़ाक रैंसिये आदि जैसे तमाम उत्तर-मार्क्सवादी चिन्तक इसी श्रेणी में आते हैं। हम देख सकते हैं कि जिन दार्शनिकों को या उत्तर-मार्क्सवादी सट्टेबाज़ दार्शनिक कहा गया है, उनकी वर्तमान राजनीतिक अवस्थिति के ईंधन का स्रोत दार्शनिक भ्रम-विभ्रम की यही भट्ठी है।
इसके अतिरिक्त, उत्तर-मार्क्सवादी सिद्धान्तकारों की ‘उग्रपरिवर्तनवादी’ प्रस्थापनाओं का राजनीतिक स्रोत यूरोपीय मज़दूर आन्दोलन के कुछ विशेष हिस्सों में, जैसे कि इटली और स्पेन के मज़दूर आन्दोलनों में उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से ही मौजूद ‘मज़दूरवाद’ (workerism) और स्वतःस्फूर्तवाद (spontaneism) की प्रवृत्तियाँ भी हैं। मार्क्सवाद-विरोधी ये पेटी-बुर्जुआ प्रवृत्तियाँ मज़दूर वर्ग की स्वतःस्फूर्तता की अन्धपूजा और आदर्शीकरण (idealization) तो करती ही हैं साथ ही मार्क्सवाद की हिरावल पार्टी की अवधारणा को ख़ारिज भी करती हैं। आज एक बार फिर दुनिया भर के और भारत के भी मज़दूर आन्दोलन में तमाम ऑटोनोमिस्ट (Autonomist), ‘मज़दूरवादी’, अराजकतावादी-संघाधिपत्यवादी ताक़तें जड़ जमाने की कोशिश कर रही हैं और अपनी इन मार्क्सवाद-विरोधी, विजातीय प्रवृत्तियों का वैचारिक ईंधन वर्तमान में उत्तर-मार्क्सवादियों के अराजकतावाद और ऑपराइज़्मो (Operaismo) की सैद्धान्तिकी से ग्रहण कर रही हैं।
उत्तर-मार्क्सवादी दर्शन के मुख्य स्रोतों की इस संक्षिप्त चर्चा के बाद हम इस विचार-सरणि के प्रातिनिधिक उदाहरण के तौर पर ऐलन बेदियू, स्लावोय ज़िज़ेक, एण्टोनियो नेग्री-माइकल हार्ट, अर्नेस्टो लाक्लाऊ-चैण्टल माउफ़ के राजनीतिक, विचारधारात्मक सैद्धान्तिकीकरणों की पड़ताल करेंगे, नये कि़स्म के कम्युनिज़्म या भविष्य की मुक्तिकामी राजनीति (emancipatory politics of future) पर उनके ”विचारों” और ”चिन्तनों” की संक्षिप्त समीक्षा करेंगे और साथ ही, बीसवीं सदी के समाजवादी प्रयोगों पर उनकी अवस्थिति का भी मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत हम ऐलन बेदियू के ‘कम्युनिज़्म’ के विचार से करेंगे।
ऐलन बेदियू का ”कम्युनिज़्म” का विचार या परिवर्तन की परियोजना से क्रान्तिकारी अभिकरण छीनने की निर्लज्ज और हताश कवायद
दार्शनिकों ने
दुनिया की तरह-तरह से व्याख्या की है
पर सवाल उसको बदलने का है।
अब चूँकि दुनिया बदलना
मेरे वश की बात नहीं
इसलिए मैं इसकी
एक और व्याख्या कर रहा हूँ
और जो थोड़ी बहुत कोशिशें हो रही हैं
दुनिया बदलने की
उनकी समीक्षा कर रहा हूँ।
– कात्यायनी (दुनिया बदलने के बारे में कतिपय सुधीजनों के विविध विचार-3)
”मार्क्सवाद, मज़दूर आन्दोलन, सामूहिक जनवाद, लेनिनवाद, सर्वहारा वर्ग की पार्टी, समाजवादी राज्य – ये सभी जो बीसवीं शताब्दी के आविष्कार हैं – अब हमारे लिए अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। सैद्धान्तिक धरातल पर ये ज़रूर अध्ययन और समीक्षा की माँग करते हैं – लेकिन व्यावहारिक राजनीति में अब ये किसी काम के नहीं रह गये हैं।”
– ऐलन बेदियू, 2008
ऐलन बेदियू और ‘कम्युनिज़्म’ के विचार-विषयक उनकी सैद्धान्तिकी पिछले कुछ समय से आम बौद्धिक हलकों में ही नहीं बल्कि वामपन्थी दायरों में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारत के कई बौद्धिक समूह और क्रान्तिकारी संगठन भी बेदियू पर चर्चा कर रहे हैं। अन्य देशों के कम्युनिस्ट ग्रुपों में भी बेदियू का सिद्धान्त चर्चा का विषय बना हुआ, बल्कि कहना चाहिए कि भ्रम का स्रोत बना हुआ है। भारत के भी कुछ अराजकतावादी-संघाधिपत्यवादी कम्युनिस्ट समूहों को बेदियू से काफ़ी-कुछ सीखने काे मिल रहा है! बेदियू ख़ुद को ‘कम्युनिज़्म की वापसी’ की उद्घाेषणा करने वाले सिद्धान्तकार के रूप में पेश कर रहे हैं। इसके चलते ही कुछ लोग इन्हें इस दौर का सबसे बड़ा ‘कम्युनिस्ट’ दार्शनिक बता रहे हैं। बेदियू 2010 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘दि कम्युनिस्ट हाइपोथीसिस’ में ही ‘कम्युनिज़्म’ के विचार संबंधी अपनी परिकल्पना (hypothesis) प्रस्तुत करते हैं, साथ ही, उक्त पुस्तक में ही वे बीसवीं सदी के समाजवादी प्रयोगों के विषय में अपनी अवस्थिति रखते हैं। इसलिए इस पुस्तक में उनके तमाम सैद्धान्तिकीकरणों की समीक्षा के ज़रिये ही हम बेदियू के ‘कम्युनिज़्म’ के विचार की वास्तविक राजनीति की विचारधारात्मक अन्तर्वस्तु तक पहुँच सकते हैं।
‘दि कम्युनिस्ट हाइपोथीसिस’ अलग से लिखी गयी कोई किताब नहीं है, बल्कि बेदियू द्वारा अलग-अलग समय पर लिखे गये लेखों या दिये गये व्याख्यानों का संकलन है। इस किताब का मुख्य स्रोत 2008 में बेदियू द्वारा ‘न्यू लेफ़्ट रिव्यू’ के लिए इसी नाम से लिखा गया वह निबन्ध है जिसमें बेदियू 2007 के राष्ट्रपति चुनावों में निकोलस सारकोज़ी की जीत के ऐतिहासिक महत्व की पड़ताल करते हैं।
इसके अलावा, मार्च 2009 में लंदन में ‘कम्युनिज़्म का विचार’ (‘दि आइडिया ऑफ़ कम्युनिज़्म’) नाम से आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में बेदियू द्वारा प्रस्तुत किया गया वक़्तव्य भी इस पुस्तक का एक स्रोत है। यहाँ बताते चलें कि इस सम्मेलन में बेदियू के अलावा स्लावोय ज़िजे़क, जुडिथ बालसो, ब्रूनो बोस्तील्स, टेरी ईगलटन, पीटर हॉलवर्ड, माइकल हार्ट, एण्टोनियो नेग्री, ज़ाक रैंसिये, एलेक्सान्द्रो रूसो, एल्बर्टो टस्कानो, जियानी वातिमो जैसे तमाम क़िस्म के मार्क्सवादियों, नव-मार्क्सवादियों और उत्तर-मार्क्सवादियों ने शिरकत की थी।
बेदियू के ‘कम्युनिज़्म’ विषयक सैद्धान्तिकीकरणों की विस्तृत समीक्षा में जाने से पहले यहाँ कुछेक बातें स्पष्ट करना आवश्यक है। पहली बात यह कि बेदियू का कम्युनिज़्म का विचार या सिद्धान्त एक गै़र-मार्क्सवादी कम्युनिज़्म की बात करता है और मार्क्सवादी विचारधारा को भविष्य की मुक्तिकामी राजनीति (emancipatory politics) के लिए अपर्याप्त, अप्रासंगिक और ग़ैर-ज़रूरी मानता है। दूसरी बात यह कि बेदियू का कम्युनिज़्म का विचार अनैतिहासिक है। बेदियू के अनुसार कम्युनिज़्म का यह विचार अनादि-अनन्त (eternal) है। यह मानवता के उद्भव के साथ ही जन्म ले चुका था। उनके लिए प्लेटो का दि रिपब्लिक, रूसो का सोशल कॉण्ट्रैक्ट, फ़्रांसीसी क्रान्ति और जैकोबिन आतंक-राज्य, पेरिस कम्यून और मार्क्सवादी कम्युनिज़्म (जो 1917 की बोल्शेविक क्रांति के साथ शुरू होता है और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के साथ ख़त्म होता है) कम्युनिज़्म के शाश्वत विचार (eternal idea) की यात्रा के अलग-अलग क्षण, पड़ाव या मील के पत्थर हैं। तीसरी बात यह कि बेदियू के अनुसार बीसवीं सदी के समाजवादी प्रयोग दुर्गति/विपदा में समाप्त हुए। उनका मानना है कि सोवियत संघ और चीन में क्रान्तियों की मुक्तिकामी सम्भावना-सम्पन्नता को पार्टी-राज्य के फ्रे़मवर्क, हिरावल पार्टी के संस्थाबद्ध नेतृत्व और समाजवादी राज्यसत्ता ने पहले बाधित किया और फिर पूरी तरह नष्ट कर दिया। और चौथी बात यह कि इस सारे ”विश्लेषण” से बेदियू इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कम्युनिज़्म के विचार और मुक्ति की राजनीति को क्रान्ति के ‘पैराडाइम’ में अवस्थित नहीं किया जा सकता है और न ही पार्टी-राज्य के फ्रे़मवर्क का ‘बन्दी’ बनाया जा सकता है। और यह भी कि ”क्रान्तियों का युग” बीत चुका है। अपनी पुस्तक ‘दि कम्युनिस्ट हाइपोथीसिस’ में बेदियू इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।
बेदियू अपनी पुस्तक की शुरुआत में कहते हैं कि 1970 की ‘लाल दशाब्दी’ के अन्त के साथ पश्चिमी पूँजीवादी देशों का कम्युनिज़्म-विरोध एक बार फिर ज़ोर-शोर के साथ सामने आया। ‘नये दर्शन’ के हिमायतियों ने समाजवादी राज्यों की ‘निरंकुशता और सर्वसत्तावाद’ पर ख़ूब शोर मचाया और बुर्जुआ संसदवाद और प्रातिनिधिक जनवाद की अच्छाइयों को गिनाना शुरू कर दिया। इस उन्मादी हर्षोल्लास के पीछे जो तर्क काम कर रहा था वह यह था कि समाजवाद, जो कि कम्युनिस्ट विचार का एकमात्र मूर्त रूप था, बीसवीं सदी में पूरी तरह विफल हो गया। इसके बाद बेदियू कहते हैं कि इसलिए विफलता के विचार पर आज ”विचार” करने की आवश्यकता है। बेदियू पूछते हैं कि जब हम कहते हैं कि कम्युनिस्ट हाइपोथीसिस (परिकल्पना) के अमलीकरण के तौर पर जो समाजवादी प्रयोग हुए, उनका अन्त ‘विफलता’ में हुआ, तो हमारा मतलब क्या होता है? क्या वे पूरी तरह से असफल हुए? क्या इसका मतलब है कि हम इस परिकल्पना को ही त्याग दें या मुक्ति की पूरी समस्या को ही तिलांजलि दे दें? बेदियू को यहाँ तक पढ़ने पर पाठक के मन में उम्मीदें जगने लगती हैं, लेकिन ये उम्मीदें ज़्यादा देर तक नहीं ठहरतीं। क्योंकि इसके बाद बेदियू जो स्वर अपनाते हैं, वह वही पुराना राग है – चूँकि बीसवीं सदी की क्रान्तियाँ पार्टी-राज्य के फ्रे़मवर्क में क़ैद थीं, इसलिए वे असफल होने के लिए अभिशप्त थीं। यह प्रश्न बेदियू यहाँ इस प्रकार उठाते हैं कि बीसवीं सदी के समाजवादी प्रयोगों ने जो रूप अपनाया और जो रास्ता अख़्तियार किया, क्या उसी में तो इस ‘विफलता’ के कारण अन्तर्निहित नहीं हैं और इसलिए ‘विफलता’ उनकी नियति थी? यहाँ यह बात जोड़नी ज़रूरी है कि इस पूरी पुस्तक में, या फिर बेदियू की अन्य सभी कृतियों में भी, बीसवीं सदी में मज़दूर वर्ग द्वारा किये गये समाजवाद के प्रयोगों को बिना किसी वैज्ञानिक-ऐतिहासिक विश्लेषण को इस्तेमाल किये ही एक ‘त्रासदी’ या ‘आपदा’ मान लिया गया है। ज़िजे़क के लेखन की तरह यहाँ भी यह नतीजा आकाशवाणी के समान (axiomatic) है।
दूसरी बात यह कि रूस और चीन में समाजवादी प्रयोगों का पतन या विफलता किस दौर में शुरू होती है, इसकी भी कोई समझदारी बेदियू के लेखन में आपको नहीं मिलेगी। पश्चिमी साम्राज्यवादी प्रोपगैण्डा मशीनरी की तरह यहाँ पर भी 1990 में सोवियत संघ के विघटन तक समाजवाद का दौर क़ायम माना जाता है! 1956 के बाद सोवियत संघ की अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक साम्राज्यवादी भूमिका और देश के अन्दर जनता के ख़िलाफ़ सामाजिक फ़ासीवादी भूमिका को ही समाजवाद के रूप में चित्रित किया जाता है। हालाँकि बेदियू के लिए कम्युनिज़्म की अपनी परिकल्पना के लिए इस ‘विफलता’ की कालिकता या स्थानिकता (temporality and spatiality) को स्पष्ट करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस परिकल्पना के अनुसार तो 1917 की बोल्शेविक क्रान्ति के साथ ही समाजवाद की ‘विफलता’ का दौर शुरू हो गया था; आख़िर इस क्रान्ति ने ही तो कम्बख़्त पार्टी-राज्य के ‘पैराडाइम’ को संस्थाबद्ध और सुव्यवस्थित किया था! इसलिए बेदियू इस पुस्तक में और अन्यत्र भी, 1917 से 1953 तक के दौर की कभी चर्चा नहीं करते। इस पूरे दौर का समाहार वह यह कह कर देते हैं कि पार्टी-राज्य ने एक नयी क़िस्म की ”निरंकुशता” को जन्म दिया जिसकी मुख्य आभिलाक्षणिकताएँ थीं- ‘पुलिस द्वारा दमन’ और ‘आन्तरिक नौकरशाहाना जड़ता’। क्या इस समझदारी पर उन्हीं आलोचनाओं की छाप नज़र नहीं आती जो अलग-अलग तरीक़े से लियॉन त्रात्स्की, रॉय मेदवेदेव, इज़ाक डॉइशर, मार्क फ़ेरो जैसे लोग करते हैं? हालाँकि इन सब में काफ़ी मतान्तर और विविधता है लेकिन रूसी क्रान्ति और समाजवादी मज़दूर सत्ता को और विशेष तौर पर स्तालिन के नेतृत्व में समाजवाद के निर्माण को कोसने में गहरी एकता है?
इसके बाद बेदियू तीन प्रकार की विफलताओं की बात करते हैं। पहली प्रकार की ‘विफलता’ वह है जिसमें क्रान्तिकारी कुछ समय के लिए किसी देश या किसी विशिष्ट इलाक़े में सत्ता पर काबिज़ होते हैं लेकिन हथियारबन्द प्रतिक्रान्तिकारी ताक़तों द्वारा कुचल दिये जाते हैं। इस ‘विफलता’ के तौर पर वह पेरिस कम्यून और रोज़ा लग्ज़मबर्ग और कार्ल लीबनेख़्त के नेतृत्व में प्रथम-विश्वयुद्ध के बाद की स्पार्टकिस्ट बग़ावत का उदाहरण देते हैं। दूसरे प्रकार की ‘विफलता’ के उपशीर्षक के तहत वे उन व्यापक जनान्दोलनों को गिनाते हैं जिनका मक़सद सत्ता हथियाना होता ही नहीं है, हालाँकि ये आन्दोलन कुछ समय के लिए राज्य की प्रतिक्रियावादी ताक़तों को रक्षात्मक मुद्रा में आने के लिए बाध्य करते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर वह मई 1968 का आन्दोलन गिनाते हैं। फिर बेदियू तीसरे प्रकार की ‘विफलता’ का चर्चा करते हैं जिसके तहत वे बिना कोई फ़र्क़ किये बीसवीं सदी के सभी समाजवादी प्रयोगों को गिनाते हैं जिनमें कम्युनिस्ट परिकल्पना के अमलीकरण के नाम पर ”पार्टी-राज्य का आतंक राज्य क़ायम हुआ” और कम्युनिज़्म के विचार को ही त्याग दिया गया! अपनी प्रस्तावना का अन्त बेदियू ”प्वाइण्ट” (बिन्दु या क्षण) की अपनी अवधारणा से करते हैं। आम तौर पर भी इस पुस्तक में जहाँ-तहाँ बेदियू उत्तर-मार्क्सवादियों की पसन्दीदा हेगेलीय दर्शन और लकानीय मनोविश्लेषण की श्रेणियों का इस्तेमाल करते नज़र आते हैं, उदाहरण के लिए बेदियू की ”ट्रूथ-प्रोसीजर”, ”इवेण्ट”, ”सब्जेक्ट” इत्यादि की अवधारणा आदि, मगर फि़लहाल हम पहले ”प्वाइण्ट” की बेदियू की अवधारणा पर विचार करते हैं। ”प्वाइण्ट” की अवधारणा को व्याख्यायित करते हुए बेदियू कहते हैं कि किसी भी मुक्तिकामी राजनीति के क्रम या श्रृंखला में (यानी कि किसी भी क्रान्ति के दौरान) यह वह क्षण होता है जिसमें विकल्प की ‘बाइनरी’ पर (यानी कि इस प्रश्न पर कि विकल्प ‘क’ अपनाया जाये या विकल्प ‘ख’) उस पूरी प्रक्रिया का भविष्य निर्भर करता है। वे आगे कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि सभी ”विफलताओं” का कारण इसी क्षण पर लिये गये फै़सलों में अन्तर्निहित है। सीधे-साफ़ शब्दों में कहें तो बेदियू के कहने का अभिप्राय यह है कि पेरिस कम्यून के अनुभवों के बाद, पहले मार्क्स और फिर लेनिन द्वारा, हिरावल पार्टी और सर्वहारा राज्य-सत्ता (सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व) की प्रस्थापनाओं का प्रतिपादन ही इस क्षण पर लिये गये ग़लत फैसले थे। यह ‘मूल पाप’ था; नाजुक मौक़े पर ग़लत फ़ैसला! और यहीं से सारी ग़लती और विफलता की शुरुआत होती है! बेदियू अपनी इसी थीसिस को इस पुस्तक के बाकी हिस्सों में स्पष्ट करते चलते हैं और हर स्पष्ट अवधारणा को इस प्रक्रिया में अस्पष्ट करते जाते हैं।
अन्यत्र बेदियू कहते हैं कि मई 1968 की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इसके बाद बेदियू मई 1968 की विजातीयता और बहुलता की बात करते हुए कहते हैं कि मई 1968 कोई एकाश्मीय परिघटना नहीं थी बल्कि चार अलग-अलग परिघटनाओं की जटिलता लिये हुए थी (बेदियू स्वयं भी इस आन्दोलन का हिस्सा थे)। पहला मई 1968 वह था जिसमें विश्वविद्यालय और स्कूलों के छात्रा-छात्राएँ हिस्सा ले रहे थे, यानी कि जिसका मुख्य तत्व छात्र-आन्दोलन था। दूसरा मई 1968 मज़दूर आन्दोलन के इर्द-गिर्द केन्द्रित था, जिसमें सी.जी.टी. (जनरल कॉनफ़ेडरेशन ऑफ़ लेबर – एक संशोधनवादी ट्रेड यूनियन संघ) और अन्य यूनियनों द्वारा आयोजित हड़तालों के साथ ही परम्परागत यूनियन के सांगठनिक ढाँचे के बाहर भी मज़दूरों द्वारा आयोजित हड़तालें थीं, जिन्हें ”वाइल्डकैट स्ट्राइक्स” की संज्ञा दी जाती थी। इस दौरान फैक्ट्रियों पर कब्ज़ा आम बात थी। तीसरे मई 1968 को स्वच्छन्तावादी (लिबर्टैरियन) मई कहा जा सकता है जिसमें पेटी बुर्जुआ वर्ग की वैयक्तिक स्वतन्त्राता का मुद्दा अहम था। इसकी अभिव्यक्ति उस दौर के कला साहित्य, सिनेमा में भी नज़र आती है। इसके बाद बेदियू चौथे मई 1968 की चर्चा पर आते हैं, जो उनके अनुसार उपरोक्त सभी से कहीं ज़्यादा ज़रूरी था। बेदियू के अनुसार यह इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह राजनीति की पुरानी क्लासिकीय अवधारणाओं पर – जैसे पार्टी, यूनियन आदि पर – सवाल उठा रहा था। इस कथन में आंशिक सच्चाई है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं 1960 के दशक से ही फ़्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी (पी.सी.एफ़.) संशोधनवाद के रास्ते पर चल चुकी थी। जहाँ तक सी.जी.टी. जैसी संशोधनवादी, अराजकतादी-संघातिपत्यवादी यूनियनों का सवाल था, तो उनकी स्थिति और अवस्थिति बहुत कुछ वर्तमान भारत में सीटू, ऐटक जैसी यूनियनों के जैसी ही थी। ऐसे में, पार्टी और यूनियनों का जो मॉडल मौजूद था, उससे मोहभंग होना लाज़िमी था और चूँकि उस समय कोई क्रान्तिकारी विकल्प मौजूद नहीं था जो इन स्वतःस्फूर्त जनउभार की कार्रवाइयों को संगठित कर सकता इसलिए मई 1968 बस मई 1968 बनकर ही रह गया। केवल विद्रोह की सफलता और असफलता की बात की जाये तो इसका अन्त उसी हताशा में हुआ, जिस हताशा में ‘ऑक्युपाई’ आन्दोलन और अरब बसन्त का हुआ है, हालाँकि मई 1968 का महत्व इस रूप में भी था कि इसके बाद तमाम ऐसी विचार-सरणियाँ पैदा हुईं जिनका अन्त ‘उत्तर’-वादी विचार-सरणियों में हो गया। इसका उल्लेख हम आलेख के पहले हिस्से में कर चुके हैं।
शायद बेदियू बिल्कुल इन्हीं कारणों से मई 1968 को लेकर इतना नॉस्टैलजिक हैं, क्योंकि मई 1968 ने पार्टी, राज्य और वर्ग अधिनायकत्व की बुनियादी अवधारणाओं पर प्रश्न उठाना शुरू किया। इस दौर में पुरानी क्लासिकीय अवधारणाओं पर खड़े हो रहे सवालों के तर्क को बेदियू बढ़ाते हुए मार्क्सवाद और क्रान्ति के विज्ञान को ख़ारिज करने तक ले जाते हैं। बेदियू कहते हैं कि ”धीरे-धीरे यह सत्य उजागर होने लगा था कि जो सामान्य भाषा, जिसका द्योतक लाल झण्डा था, हम सब बोल रहे थे, वह दरअसल मृत्यु को प्राप्त हो रही थी।” मई 1968 की असली अहमियत बेदियू के लिए यहाँ छिपी है।
बेदियू जैसे तमाम उत्तर-मार्क्सवादियों का हमला मूलतः मार्क्सवाद की क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तु पर है। इस विषय में बेदियू की स्पष्टवादिता की दाद देनी पड़ेगी कि वह सीधे-सीधे यह कह भी देते हैं कि मार्क्सवाद, पार्टी और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की सोच पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुकी है। चीन में 1966 में शुरू हुई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति का भी बेदियू एक ग़ैर-पार्टीवादी विनियोजन करते हैं। बेदियू के अनुसार महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के साथ जो नया युग शुरू हुआ उसमें पार्टी-राज्य का फ्रे़मवर्क (यानी हिरावल पार्टी और सर्वहारा तानाशाही की मार्क्सवादी अवधारणाएँ) अब बेकार हो चुका है। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति पर बेदियू के विचारों की चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ इस बात को रेखांकित करना ज़रूरी है कि मार्क्सवादी कम्युनिज़्म के बरक्स बेदियू के ”कम्युनिज़्म” के काण्टीय, हेगेलीय, लकानीय विचार के बावजूद, और शायद इसी वजह से, भी उनका निशाना एकदम ठीक वे अवधारणाएँ हैं जो मार्क्सवाद की क्रान्तिकारी अर्न्तवस्तु का निर्माण करती हैं।
राजनीतिक अर्थशास्त्र की बेहद अधकचरी और सीमित समझदारी का परिचय भी बेदियू जहाँ-तहाँ अपने लेखन में देते चलते हैं। मसलन, बेदियू एक जगह कहते हैं कि वित्तीय पूँजीवाद पिछले 500 सालों से पूँजीवाद का एक केन्द्रीय संघटक अवयव रहा है! साम्राज्यवाद के ग़ैर-लेनिनवादी अध्येता और आम अकादमिक शोधकर्ता भी इस तरह की बचकानी प्रस्थापनाएँ नहीं देते हैं! मार्क्सवादी-लेनिनवादी विज्ञान को तो बेदियू ने पहले ही इतिहास की कचरा-पेटी के हवाले कर दिया है। हालाँकि कोई ग़ैर-मार्क्सवादी भी उपनिवेशवाद के प्राक्-वित्तीय दौर और वित्तीय दौर में फ़र्क़ करेगा, लेकिन बेदियू ऐसा नहीं कर पाते। क्योंकि, लकाँ और हेगेल के पोथों के बीच ही वे दब-से गये हैं! वैसे, सभी उत्तर-मार्क्सवादी चिन्तकों के बारे में एक बात दावे से कही जा सकती है – इन्हें राजनीतिक अर्थशास्त्र का ‘क ख ग’ भी नहीं आता है। इस कमी को इतिहास की सुसंगत जानकारी और एक सन्तुलित ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव के रूप में भी देखा जा सकता है। और कमी को ये बेदियू पूरा कैसे करते हैं? फ़्रांसीसी फ़ैशनेबल उत्तर-वाम की लच्छेदार शब्दावली में ऐतिहासिक तथ्यों के विकृतीकरण के अद्वितीय हुनर के ज़रिये! आमतौर पर बेदियू इतिहास के प्रति अवहेलना का दृष्टिकोण ही अपनाते हैं। लेकिन अपने राजनीतिक-दार्शनिक हित-साधन के लिए वह आत्मगत चयन करते हुए ऐतिहासिक तथ्यों का ब्यौरा देने से बाज़ नहीं आते हैं। वह इन तथ्यों को इस तरह तोड़-मरोड़ कर और मनमाने ढंग से पेश करते हैं कि उनकी अन्तर्वस्तु ही बदल जाती है। मसलन, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति पर अपने विचार रखते हुए वे जमकर तथ्यों का ब्यौरा देते हैं, लेकिन यह आत्मगत पूर्वाग्रहों के साथ किया गया इतिहास का एक पाठ है, जिसमें नतीजे पहले ही तय कर लिये गये हैं और उनके आधार पर तथ्यों का चयन बाद में किया गया है।
बेदियू अपने लेखन में एक टटपुँजिया स्वच्छन्दतावादी की तरह (जो कि वह हैं!) रूमानीपन का प्रदर्शन करते हैं और छद्म आशावाद से ग्रस्त होकर कहते हैं कि आज सबसे अहम है विचारों और एक सामान्य परिकल्पना के प्रति अपने जुनून को एक बार फिर तलाशना (!), इस विश्वास के साथ की एक दूसरी दुनिया सम्भव है! ”हमें पूँजीवाद के घृणित तमाशे के बरक्स लोगों का, लोगों के जीवन का और विचारों के आन्दोलन का यथार्थ खड़ा करना होगा।” यह कैसे खड़ा होगा यह बताना बेदियू ज़रूरी नहीं समझते लेकिन अपनी पुरानी थीम पर वह ज़रूर एक बार फिर लौटते हैं (ऐसा करना वह कभी नहीं भूलते!)। वे कहते हैं कि हालाँकि ‘कम्युनिज़्म’ शब्द को ”सस्ता और वेश्या बना दिया गया है” लेकिन हम इसे लुप्त नहीं होने देंगे। चूँकि बेदियू ”कम्युनिज़्म” के इस विचार के तारणहार हैं, इसलिए वह ”कम्युनिज़्म” को बचाएँगे! एलेन बेदियू उसे अतीत के सारे अनुभवों से, क्रान्ति के सिद्धान्त से, समाजवादी राज्य से और हिरावल पार्टी के भारी-भरकम बोझ से इस ”शाश्वत” विचार को भारमुक्त करेंगे और ”मुक्ति की नयी राजनीति” गढ़ेंगे, जो क्या होगी यह बेदियू नहीं बताएँगे क्योंकि वह ख़ुद भी इससे अपरिचित हैं!
अपने उत्तरमार्क्सवादी चिन्तन से पैदा हुए पूर्वाग्रहों के चलते बेदियू माओ का, माओवाद का और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति का निकृष्ट क़िस्म का हस्तगतीकरण (appropriation) और विकृतीकरण (distortion) करते हैं। वह कहते हैं कि सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति पार्टी-राज्य के स्वरूप के संतृप्तीकरण (saturation) का प्रारूपिक उदाहरण है। इसके बाद वे जोड़ते हैं कि हालाँकि यह स्वयं (सांस्कृतिक क्रान्ति) पार्टी-राज्य के फ्रे़मवर्क के भीतर ही काम कर रही थी और इसीलिए ”विफल” हुई, लेकिन इसने आने वाले दिनों के लिए कुछ ज़रूरी सबक़ दिये। बेदियू के अनुसार यह ज़रूरी सबक थे – सर्वहारा वर्ग की हिरावल पार्टी और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के मार्क्सवादी सिद्धान्त को तिलांजलि देने की वांछितता। अपने इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए बेदियू सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दौर की कई घटनाओं का ब्यौरा टुकड़ों-टुकड़ों में देते हैं, मनमाने ढंग से उन घटनाक्रमों की व्याख्या करते हैं और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति की क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तु का विकृतीकरण करते हैं।
बेदियू माओ का पेटी बुर्जुआ लोकरंजकतावादी विनियोजन करके उन्हें हिरावल पार्टी की अवधारणा के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास करते हैं। हालाँकि यह दीगर बात है कि इस उपक्रम में वह कोई विशेष सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति की क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तु को समझने की उम्मीद हम बेदियू जैसे उत्तर-मार्क्सवादी और उत्तर-माओवादी (क्योंकि बकौल बेदियू पार्टी-राज्य फ़्रेमवर्क की कै़द से कम्युनिज़्म के विचार को मुक्त कराने में वे माओ से भी आगे निकल गये हैं!) से कर भी नहीं सकते हैं। इस अध्याय के अन्त में वे कहते हैं, ”आज हम जानते हैं कि हर क़िस्म की मुक्तिकामी राजनीति को पार्टी के मॉडल के आगे सोचना होगा और पार्टी-राज्य के फ़्रेमवर्क के अध्याय को अन्तिम और निर्णायक तौर पर बन्द कर देना होगा। भविष्य की राजनीति पार्टी के बिना होगी…” लेकिन, भविष्य की यह राजनीति क्या होगी, बेदियू एक बार फिर इस प्रश्न पर चुप्पी साधे हुए हैं।
बेदियू अपनी रचनाओं में पेरिस कम्यून के मॉडल का खूब समर्थन करते हैं। कारण स्पष्ट है – क्योंकि पेरिस कम्यून के वक़्त हिरावल पार्टी और सर्वहारा राज्य की अवधारणा उतनी सुस्पष्ट नहीं थी जितना कि मज़दूर वर्ग के राजनीतिक सत्ता पर क़ाबिज़ होने के इस पहले प्रयोग के समाहार के बाद वह हुई। बेदियू के शब्दों में कहें तो कम्यून पार्टी-राज्य फ़्रेमवर्क का बन्दी नहीं था। मार्क्स ने कम्यून की परिस्थितियों, कारणों और अनुभवों का निचोड़ निकालते हुए जो निष्कर्ष निकाला, उसे भी याद करना यहाँ ज़रूरी है। मार्क्स ने कहा था, ”मज़दूर वर्ग बनी-बनायी राज्य मशीनरी को ज्यों का त्यों हाथ में नहीं ले सकता और उसे अपना मक़सद पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता।” उन्होंने बताया कि सर्वहारा वर्ग को पुरानी राज्य मशीनरी को ”तोड़ने” और ”चकनाचूर करने के लिए” क्रान्तिकारी हिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए तथा ”सर्वहारा अधिनायकत्व” को लागू करना चाहिए। बेदियू का कहना कि मार्क्स कम्यून के अपने आकलन में सुस्पष्ट नहीं थे, कोरी लफ़्फ़ाज़ी है। उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि सर्वहारा राज्यसत्ता के विषय में मार्क्स के विचार वास्तव में क्या थे। यह बेदियू का स्वतःस्फ़ूर्ततावाद और पार्टी-राज्य फ़्रेमवर्क से उनकी ‘एलर्जी’ है जो उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुँचाती है। बेदियू के अनुसार एक दूसरी दुनिया का भ्रूण कम्यून के मॉडल में ही आकार ले रहा है क्योंकि यह मॉडल पार्टी-राज्य के स्वरूप से मुक्त है। यह इतिहास के चक्के को पीछे धकेलना नहीं तो और क्या है? पेरिस कम्यून का प्रयोग ठीक यही दिखलाता था कि सर्वहारा वर्ग को क्रान्तिकारी विचारधारा और क्रान्तिकारी संगठन की आवश्यकता है और उनके ज़रिये ही वह बुर्जुआ राज्यसत्ता का ध्वंस कर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को क़ायम कर सकता है। मज़दूर वर्ग व अन्य मेहनतकश वर्गों के विरुद्ध हिंसा के संगठित उपकरण का ध्वंस संगठित क्रान्तिकारी हिंसा के ज़रिये ही किया जा सकता है। लेकिन बेदियू के लिए पेरिस कम्यून का मॉडल राज्य, पार्टी आदि की अशुद्धताओं से मुक्त था! यह तथ्यतः भी ग़लत है। दस सप्ताह से कुछ ज़्यादा समय तक पेरिस में मज़दूरों की सत्ता ने जो कुछ किया वह क्रान्तिकारी हिंसा और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व ही था! बल्कि, मार्क्स के शब्दों को उधार लेते हुए कहा जा सकता है कि भ्रूण रूप में सर्वहारा सत्ता और शासन का एक नमूना पेश करने के बावजूद, पेरिस कम्यून की सबसे बड़ी ग़लती यही रही कि उसने क्रान्तिकारी हिंसा और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को पर्याप्त हद तक लागू नहीं किया। लेकिन बेदियू हर ऐतिहासिक घटना की तरह पेरिस कम्यून का ज़िक्र करते हुए भी मनमाने ढंग से तथ्यों का चयन और व्याख्या करते हैं ताकि अपनी पैथोलॉजिकल प्रतिक्रिया को और राजनीतिक सदमे को अभिव्यक्ति दे सकें। बेदियू का काम आसान है : नतीजे पहले से तय हैं, बस तथ्यों को उसमें फिट करना है।
बेदियू के ”कम्युनिज़्म” का विचार क्या है, इसकी चर्चा हम पहले कर आये हैं। अपने ”कम्युनिज़्म” के विचार को परिभाषित करने के लिए बेदियू यथार्थ (the Real), काल्पनिक (the Imaginary) और प्रतीकात्मक (the Symbolic) की लकानियन त्रयी को लागू करते हैं। उनके अनुसार इतिहास ‘प्रतीक’ का क्षेत्र है, भविष्य की परियोजना (उनके लिए कम्युनिज़्म का विचार) ‘काल्पनिक’ का क्षेत्र है और राजनीति ‘यथार्थ’ का क्षेत्र है! आप इस बँटवारे के पीछे बेदियू की पूरी हेगेलीय-लकानीय समझदारी को देख सकते हैं। यदि कम्युनिज़्म की परियोजना ‘काल्पनिक’ का क्षेत्र है तो कम्युनिज़्म की पूरी परियोजना एक आत्मगत कारक बन जाती है। इसके अलावा बेदियू का कम्युनिज़्म एक काण्टीय नियामक विचार (Regulative Idea) है जिसके लिए यथार्थ के अनुरूप होना या उसका प्रतिनिध्त्वि करना अनिवार्य नहीं है। यह एक लोकोत्तर विचार (transcendental Idea) है। इसलिए बेदियू के कम्युनिज़्म का विचार महज़ एक विचार है, यह किसी क़िस्म के अमलीकरण या मूर्तीकरण का मोहताज नहीं है! ऐसा क्यों है इसे हम आगे स्पष्ट करेंगे।
बेदियू मार्क्सवाद पर हमला करने के लिए ज़ाक लकाँ के मनोविश्लेषण की श्रेणियों का इस्तेमाल एक विशेष उद्देश्य से करते हैं। इस प्रच्छन्न उद्देश्य को समझने के लिए हमें कुछ शब्द लकाँ की इन श्रेणियों को समझने पर ख़र्च करने पड़ेंगे, अन्यथा बेदियू के असली मन्तव्य और मंशा को सही ढंग से समझा नहीं जा सकता है। यह कुछ साथियों को थोड़ा उबाऊ या ग़ैर-ज़रूरी लग सकता है। लेकिन इन उत्तर-मार्क्सवादियों का हमला मार्क्सवाद पर इसी प्रकार का है कि असल बात तक पहुँचने से पहले लफ़्फ़ाज़ियों के कई पर्दों को चीरना पड़ता है। इसके बिना बेदियू जैसे उत्तर-मार्क्सवादियों की सुसंगत आलोचना मुश्किल है, और किसी भी प्रकार की यान्त्रिक या चलताऊ आलोचना मार्क्सवाद के उद्देश्य को लाभ के बजाय हानि ही पहुँचाती है। हम इसे अधिकतम सम्भव सहज और सरल रूप में रखने का प्रयास करेंगे, ताकि बुनियादी बात को समझकर बेदियू की आलोचना पर आगे बढ़ सकें। हम आपको यक़ीन दिलाते हैं इस छोटे-से बोझिल पैराग्राफ़ के बाद हम बेदियू द्वारा मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धान्तों पर हमले के मूल को देख सकेंगे!
कम्युनिज़्म के विचार को ‘काल्पनिक’ के रूप में, इतिहास को ‘प्रतीकात्मक’ के रूप में और राजनीतिक को ‘यथार्थ’ के रूप में चित्रित करने के पीछे भी जो सोच काम कर रही है, वह क्या है और इसके पीछे बेदियू का मक़सद क्या है? इसके अनुसार, इतिहास ‘प्रतीकात्मक’ का प्रतिनिधित्व करता है। लकानीय त्रयी में अगर हम ‘यथार्थ’, ‘प्रतीकात्मक’ और ‘काल्पनिक’ के सम्बन्ध को समझ लें तो बेदियू का हेगेलीय भाववाद खुलकर सामने आ जाता है। मनुष्य के मनोविज्ञान के निर्माण की व्याख्या करते हुए लकाँ ने कहा कि ‘यथार्थ’ (the Real) ‘वास्तविकता’ (the reality) से अलग वस्तु है। ‘यथार्थ’ वह स्थिति है जिससे हम उस क्षण हमेशा के लिए काट दिये जाते हैं, जिस दिन हम भाषा के जगत में प्रवेश करते हैं। यानी कि अपनी छवि के प्रति सचेत होने के पहले एक नवजात शिशु ‘यथार्थ’ के जगत में होता है। इस मंज़िल में बच्चा सिर्फ़ आवश्यकता और उसकी पूर्ति को पहचानता है। वह अभी अपने, अपनी माँ या बाह्य जगत में अन्तर नहीं जानता है। लकाँ के लिए यह मंज़िल पूर्णता (completeness या fullness) की मंज़िल है। यह बोध भाषा में बच्चे के प्रवेश के साथ खो जाता है। भाषा के जगत में प्रवेश करते ही आवश्यकता (necessity) माँग (demand) बन जाती है। यथार्थ से यह अलगाव स्थायी होता है और इसीलिए लकाँ का कहना था कि मनुष्यों के लिए यथार्थ असम्भव है, क्योंकि इसे भाषा में अभिव्यक्त ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन लकाँ के मुताबिक़ यथार्थ हमेशा एक भूमिका अदा करता रहता है और ‘काल्पनिक’ और ‘प्रतीकात्मक’ ‘यथार्थ’ के पत्थर से बार-बार टकराते हैं और असफल होते रहते हैं। ‘काल्पनिक’ से लकाँ का क्या अभिप्राय है? ‘काल्पनिक’ की अवस्था ‘मिरर स्टेज’ की अवस्था है जिसमें सब्जेक्ट (व्यक्ति) आदिम आवश्यकता से ”माँग” की मंज़िल में प्रवेश करता है। आवश्यकता पूरी हो सकती है, लेकिन ”माँग” कभी पूरी नहीं हो सकती है। इसकी वजह से एक ‘अभाव/कमी’ का बोध जन्म लेता है। जैसे ही किसी को अपने अस्तित्व के दुनिया से अलग होने का पता चलता है वैसे ही एक अकुलाहट की भावना जन्म लेती है, जिसके पीछे कुछ ‘खो’ जाने का बोध काम करता है। बच्चा जैसे ही इस मंज़िल में पहुँचता है, उसकी ”माँग” होती है इस अन्यता (otherness) के घेरे में आ चुकी दुनिया को अपना अंग बनाना, जैसा कि बच्चे की नवजात अवस्था में हुआ करता था, जब बच्चा भाषा में प्रवेश के साथ अपने आपको दुनिया से अलग नहीं देखता था। यह ”माँग” अपूरणीय होती है, क्योंकि यह उस छवि (image) पर आधारित है जो बच्चे ने अपने मन में बनायी है; यह छवि सुसंगत है, पूर्ण है, और स्थिरतापूर्ण है, लेकिन यह छवि उस वास्तविक बच्चे जैसी नहीं है। यह छवि एक कल्पना है जो बच्चे ने अपनी माँग के आधार पर बनायी है और इस रूप में अपूरणीय है। यह छवि किसी भी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो कि बच्चा बनना चाहता हो; और इस रूप में अपनी ‘काल्पनिक’ छवि से उसका सम्बन्ध नारसिसिस्टिक है। अब आते हैं लकाँ के ‘प्रतीकात्मक’ के सिद्धान्त पर। ‘प्रतीकात्मक’ वास्तव में ‘काल्पनिक’ की सहायता से और भाषा के माध्यम के जि़रये ‘यथार्थ’ की एक श्रेणीबद्ध प्रस्तुति है। मिसाल के तौर पर, ‘काल्पनिक’ के विश्व में हम अच्छे-बुरे, दुख-आनन्द, आदि के बारे में आदर्शीकृत धारणाएँ रखते हैं और अच्छा बुरे का, दुख आनन्द का बहिष्कार करता है; उनमें से एक ही स्वीकार्य होता है; यह वह धरातल होता है जहाँ हम चयन करते हैं। लेकिन ‘प्रतीकात्मक’ के जगत में इन दोनों का अस्तित्व सम्भव होता है; हालाँकि उनके बीच हम भेद करते हैं, मगर हम उन दोनों के अस्तित्वों को स्वीकार करते हैं। ‘यथार्थ’ में ऐसी श्रेणियाँ होती ही नहीं हैं; चूँकि ‘यथार्थ’ उस दौर का प्रतिनिधित्व करता है जब/जहाँ भाषा नहीं थी और इसलिए विचारधारा भी नहीं थी। बाद में, भाषा के प्रवेश के साथ और अपनी ‘कल्पनाओं’ की श्रेणियों की सहायता से हम ‘यथार्थ’ का ‘वास्तविकता’ के रूप में पुनरुत्पादन करते हैं। यह सारा झमेला दरअसल यह कह रहा है कि ‘काल्पनिक’ मानसिक निर्मिति है, जो कि भाषा के जगत में प्रवेश के समय ‘स्व’ और ‘अन्य’ में भेद के साथ पैदा होती है; इस दौर के पहले ‘स्व’ और ‘अन्य’ एक व पूर्ण होते हैं और यह ‘यथार्थ’ की मंज़िल होती है; इसके बाद, भाषा (विचारधारा) के माध्यम से हम ‘यथार्थ’ को समझने के प्रयास में उसे श्रेणीबद्ध करते हैं, उसे समझने के लिए विभेदीकृत करते हैं (जो कि दरअसल ‘यथार्थ’ होता ही नहीं है!) और इस प्रक्रिया में अपने लिए एक ‘वास्तविकता’ का निर्माण करते हैं जो कि एक निर्मिति ही होती है और यही ‘प्रतीकात्मक’ का आधार है! यथार्थ अज्ञेय है! और इसीलिए जैसे ही हमारा ‘काल्पनिक’ और ‘प्रतीकात्मक’ इस ‘यथार्थ’ से टकराते हैं, वैसे ही वे छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, और इसके साथ ही नये ‘काल्पनिक’ और नये ‘प्रतीकात्मक’ की रचना होती है, जो एक नयी ‘वास्तविकता’ के रूप में एक नयी निर्मिति का निर्माण करते हैं, जो कि और कुछ नहीं बल्कि ‘यथार्थ’ की एक छद्म प्रस्तुति ही होती है।
अब ज़रा याद करें कि बेदियू ने अपने कम्युनिज़्म के विचार की बात करते हुए इस लकानियन त्रयी में किसे क्या कहा है – इतिहास ‘प्रतीकात्मक’ का प्रतिनिधित्व करता है; कम्युनिज़्म का विचार ‘काल्पनिक’ का प्रतिनिधित्व करता है; और राजनीति ‘यथार्थ’ का प्रतिनिधित्व करती है! यानी कि इतिहास भाषा और पाठ का क्षेत्र है, वास्तव में इतिहास (‘ऐसा हुआ था’) का कोई अस्तित्व नहीं है, यह आपकी कल्पनाओं की मदद से इतिहास की भाषाई निर्मिति है! कम्युनिज़्म का विचार कल्पनाओं का क्षेत्र है जिसमें मानवता अपनी वह ”माँग” रखती है, जो कि एक आदर्श मनोगत छवि और यथार्थ के टकराव या विरोध से पैदा हुई है, और जो ठीक इसीलिए पूर्ण नहीं हो सकती; नतीजतन, इस ”माँग” को शाश्वत रूप से (eternally) यथार्थ से टकराते रहना है, भंग होते रहना है और पुनर्निर्मित होते रहना है! कम्युनिज़्म के विचार की यह अनन्त यात्रा है, जिसमें अब पुरानी ”माँगें” (पार्टी, राज्य, वर्ग आदि) यथार्थ से टकरा कर भंग हो चुकी हैं और अब नयी ”माँगें” यथार्थ के साथ नये द्वन्द्व में निर्मित हो रही हैं और ”इच्छाओं” के रूप में अपने आपको भाषा/विचारधारा में अभिव्यक्त कर रही हैं। और यथार्थ क्या है? वह समकालीन राजनीति है जिसकी संरचना को भाषा या विचारधारा में नहीं बाँधा जा सकता है; यह ‘यथार्थ’ भाषा-पूर्व युग की वस्तु है और भाषा में कल्पना के सहारे इसकी निर्मिति उसकी छद्म प्रस्तुति ही होगी, एक ‘वास्तविकता’ का निर्माण होगा! तो फिर आप राजनीति सचेतन तौर पर और योजनाबद्ध रूप में करें क्या? बेदियू का जवाब सीधा है – कुछ नहीं! यह यथार्थ स्वायत्त रूप से विकसित होना है और इसमें जो बदलाव होंगे उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और यहीं से हम बेदियू के कुछ अन्य निष्क्रिय उग्रपरिवर्तनवादी प्रतिपादनों पर आ सकते हैं, जिसमें सबसे अहम है ”इवेण्ट” की अवधारणा। बेदियू के ”इवेण्ट” (घटना/संयोग) की अवधारणा के अनुसार समाज में होनेवाले सभी बदलाव आकस्मिक होते हैं और उनका सैद्धान्तिकीकरण नहीं किया जा सकता। अब आप इस बात को बेदियू की ‘यथार्थ’ की अवधारणा से जोड़ सकते हैं। चूँकि यथार्थ सैद्धान्तिकीकरण से परे है (क्योंकि सैद्धान्तिकीकरण का माध्यम भाषा और पाठ है) इसलिए यथार्थ में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी कुछ पहले से नहीं कहा जा सकता, उनका सैद्धान्तिकीकरण नहीं किया जा सकता और इन्हीं परिवर्तनों को व्याख्यायित करने के लिए ”इवेण्ट” की अवधारणा बेदियू द्वारा रची गयी है। यह ”इवेण्ट” ही नयी सम्भावनाओं को जन्म देता है, लेकिन ”इवेण्ट” का होना संयोग या इत्तेफ़ाक की बात है, इसलिए आमूलगामी सामाजिक परिवर्तन की पूरी परियोजना ही बेदियू द्वारा संयोग के क्षेत्र में धकेल दी गयी है। इसमें सचेतन योजना और राजनीति का स्थान नहीं है या अगर है तो वह एक निष्प्रभावी स्वतःस्फ़ूर्ततावादी उपस्थिति है। और इस तरह से क्रान्ति या कहें कि परिवर्तन से हर प्रकार का अभिकरण छीन लिया गया है। क्योंकि किसी सचेतन अभिकर्ता की आवश्यकता ही नहीं है! इसी निष्क्रिय उग्रपरिवर्तनवाद की मदद के लिए एक अन्य सैद्धान्तिकीकरण जो बेदियू यहाँ प्रस्तुत करते हैं वह है उनका ”सबट्रैक्शन” (व्यवकलन) का सिद्धान्त। इसके अनुसार आज कम्युनिज़्म का लक्ष्य राज्य का विलोपीकरण नहीं है (क्योंकि यह एक असीमित, अपरिमित प्रक्रिया है!), बल्कि ”राज्य से दूरी बनाये रखने की राजनीति” है – जो किसी भी राज्य में किसी भी रूप में सम्मिलित होने को नकारती है। ”सबट्रैक्शन” के अपने सैद्धान्तिकीकरण के ज़रिये एक बार फिर बेदियू सर्वहारा अधिनायकत्व की अवधारणा पर हमला करते हैं और दरअसल क्रान्ति करने के सिद्धान्त पर ही हमला बोलते हैं।
”कम्युनिज़्म” की अपनी परिकल्पना और विचार के नाम पर बेदियू मार्क्सवाद की बुनियादी प्रस्थापनाओं और क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तु को ख़ारिज करने का काम करते हैं। वह अतीत के सभी समाजवादी प्रयोगों पर ”विफलता”, ”त्रासदी” और ”आपदा” का लेबल तो चस्पाँ कर देते हैं, जो कि बेदियू के लिए आकाशवाणी-समान सत्य है, लेकिन न तो उन प्रयोगों का कोई आलोचनात्मक मूल्यांकन पेश करते हैं और न ही सामाजिक परिवर्तन का अपना कोई सकारात्मक मॉडल पेश करते हैं। इस पूरे उत्तरमार्क्सवादी उपक्रम का असली मक़सद है अति-आमूलगामी शब्दावली में आमूलगामिता की हर सम्भावना या समझदारी पर चोट की जाये और इसीलिए उनके हर सिद्धान्त का असल निशान मार्क्सवाद की क्रान्तिकारी कोर अन्तर्वस्तु यानी कि वर्ग, राज्य, और पार्टी का सिद्धान्त है।
‘कम्युनिज़्म एब्सकॉण्डिटस’ या स्लावोय ज़िज़ेक के निठल्ले, निष्क्रिय, नुक़सानदेह सैद्धान्तिकीकरण का नया उदाहरण
दार्शनिकों ने
दुनिया की तरह-तरह से व्याख्या की है
पर सवाल उसको बदलने का है,
मानता हूँ।
मेरे लिए मगर मुमकिन नहीं रह गया है,
बदलना इसे।
इसलिए अब मैं
सलाहकार बन गया हूँ
दुनिया बदलने वालों का
आओ दुनिया बदलने वालो!
मेरे अनुभव का लाभ उठाओ,
अन्यथा बदलते रह जाओगे
नहीं बदलेगी यह दुनिया।
– कात्यायनी (दुनिया को बदलने के बारे में कतिपय सुधीजनों के विविध विचार-2)
स्लावोय ज़िज़ेक का ज़िक्र आम तौर पर अन्तरराष्ट्रीय वाम के ‘सुपरस्टार’ दार्शनिक के रूप में होता है। वह अपनी फैशनेबल उत्तर-मार्क्सवादी, लकानियन, हेगोलियन अभिव्यक्ति शैली के कारण भी काफ़ी प्रचलित हैं। समकालीन पूँजीवादी सांस्कृतिक परिदृश्य पर उनकी टिप्पणियों या आलोचना को देखें, तो बेशक कई अन्तर्दृष्टियाँ मिलती हैं, और इस मायने में, एक सांस्कृतिक समालोचक (cultural critic) के रूप में, ज़िज़ेक उम्दा भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा, उनके ज़्यादातर सैद्धान्तिकीकरणों की वास्तविक अर्न्तवस्तु में नयापन बस नाम के लिए ही है। ज़िज़ेक के पास एक सशक्त रूप है, जिसका वह कुशलता के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वह इसका इस्तेमाल ऐसी बातें कहने में करते हैं, जो आमतौर पर सैद्धान्तिक रूप से बेहद दरिद्र, कई बार तथ्यात्मक तौर पर ग़लत, और ख़राब क़िस्म के सार-संग्रहवाद की मिसालें होती हैं। आलेख के इस भाग में हम स्लावोय ज़िज़ेक के राजनीतिक-विचारधारात्मक सैद्धान्तिकीकरणों पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालेंगे और उनकी पड़ताल करेंगे। साथ ही, हमारा ध्यान मुख्य तौर पर इस बात पर होगा कि ज़िज़ेक अपने तमाम (मार्क्सवाद से ज़्यादा!) रैडिकल दावों के बाद अन्त में क्या सकारात्मक प्रस्ताव हमारे सामने रखते हैं।
स्लावोय ज़िज़ेक के चिन्तन और रचना कर्म की एक ख़ास विशेषता है उनके चिन्तन और लेखन में किसी भी संगति और सामंजस्य का अभाव। 1989 में अंग्रेजी में प्रकाशित उनकी पहली पुस्तक ‘दि सब्लाइम ऑबजेक्ट ऑफ़ आइडियॉलोजी’ से लेकर पिछले वर्ष के उत्तरार्द्ध में प्रकाशित ‘दि इयर ऑफ़ ड्रीमिंग डेंजरसली’ तक की यात्रा में ज़िज़ेक ने कई विचारधारात्मक कलाबाज़ियाँ और गुलाटियाँ मारी हैं। शुरुआत में वह ‘उग्रपरिवर्तनवादी जनवादी परियोजना (Radical Democratic Project) की अवस्थिति पर खड़े थे जो अब मार्क्सवादी कम्युनिज़्म (ज़िज़ेक के अनुसार) में तब्दील हो चुकी है। स्लावोय ज़िज़ेक की पिछले डेढ़ दशकों के दौरान लिखी गयी रचनाओं को पढ़कर बरबस ही फ़ेदिन के उपन्यास ‘आग्नेय वर्ष’ के चरित्र त्स्वेतख़िन की याद आती है जो बोल्शेविक क्रान्ति के दौरान व्यावहारिकता के तकाज़े से पक्ष चुन रहा था और आवश्यकतानुसार पक्ष बदल भी रहा था। वैसे ज़िज़ेक के कम्युनिज़्म का यह विचार कितना मार्क्सवादी है, इसकी पड़ताल हम आगे करेंगे। ज़िज़ेक के उत्तर-मार्क्सवादी चिन्तन की अपनी समालोचना का दायरा हम मुख्यतः उनकी दो पुस्तकों में प्रस्तुत विचारों तक सीमित रखेंगे – ‘फ़र्स्ट ऐज़ ट्रेजडी, दैन ऐज़ फ़ार्स’ और ‘दि इयर ऑफ़ ड्रीमिंग डेंजरसली’। राजनीति और विशेषकर भविष्य की राजनीति से जुड़े ज़िज़ेक के सैद्धान्तिकीकरण, मुख्य तौर पर इन दो पुस्तकों में उभरकर सामने आ जाते हैं। एक बात जो ज़िज़ेक के लेखन में आपको आमतौर पर दिख जायेेगी, वह है अपने विश्लेषण के दौरान वे बेहद बेतुकी दिखने वाली तुलनाएँ करते हैं और उनमें समानताएँ तलाशने की लॉटरी खेलते हैं। मिसाल के तौर पर, ज़िज़ेक अगर कीर्केगार्द, मार्क्स और हेनरिख़ हाइने की तुलना करें तो आपको अचम्भित नहीं होना चाहिए। वह ऐसी तुलनाओं के ज़रिये जो करते हैं, वह और कुछ नहीं बल्कि ऐसी सामान्य परिघटनाओं का जटिल प्रस्तुतिकरण है, जिन्हें अन्य विचारकों, विशेष तौर पर मार्क्सवादी विचारकों, ने पहले ही सही ढंग से व्याख्यायित किया है। ऐसे प्रस्तुतिकरण के लिए वे हेगेलीय और लकाँवादी दार्शनिक और वैचारिक श्रेणियों का इस्तेमाल करते हैं। इन श्रेणियों के अतिरिक्त ज़िज़ेक सार-संग्रहवादी तरीके से किसी भी प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक या समकालीन विचारक की अवधारणाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं – ताओ, बुद्ध और प्लेटो से लेकर लॉक और देकार्त तक; काण्ट, कीर्केगार्द, अडोर्नो, वॉल्टर बेंजामिन और हाइडेगर से लेकर देल्यूश, नेग्री, हार्ट, बेदियू और जुडिथ बटलर तक। हालाँकि, इन अवधारणाओं में आम तौर पर कुछ भी सामान्य/साझा नहीं होता। इस प्रकार के तर्क से ज़िज़ेक लगातार अलग-अलग दार्शनिक व्यवस्थाओं में समानान्तर रेखाएँ खींचते रहते हैं और फिर इन समानान्तर रेखाओं का इस्तेमाल समकालीन परिदृश्य की व्याख्या करने के लिए करते हैं। इस तरीके से अलग-अलग जगहों से अलग-अलग तत्वों को अन्दाज़े से जोड़ने और जोड़कर उसे अपनी समकालीनता की व्याख्या में बिठाने को हम सट्टेबाज़ दार्शनिक पद्धति (स्पेक्युलेटिव फ़िलोसॉफ़िकल मेथड) कह सकते हैं। लेकिन यह विश्लेषण अन्त में कहीं नहीं ले जाता है, और वास्तव में यह दुनिया बदलने की बात तो बहुत दूर, दुनिया की एक आंशिक तौर पर सही व्याख्या भी नहीं होती है। कुल मिलाकर, लकाँ के मनोविश्लेषण, लेवी स्ट्रॉस के उत्तरसंरचनावाद, उत्तरआधुनिकतावाद और तमाम अन्य मार्क्सवाद-विरोधी विचार-सरणियों से मिलने वाली जूठन का इस्तेमाल करते हुए इनका दर्शन अपने आपको मार्क्स से ज़्यादा रैडिकल दिखलाने का प्रयास करता है, और लगातार यह दिखाने का प्रयास करता है कि मार्क्स क्या-क्या नहीं समझ पाये और कहाँ-कहाँ वह ग़लत थे।
साथ ही एक और बात जो ज़िज़ेक के चिन्तन की आभिलाक्षणिकता है वह है उनका ख़ुद को ‘लेनिनवादी’ क़रार देते रहना। वह बार-बार इस बात पर शोर देते हैं कि आज लेनिन को ‘दोहराये’ जाने की ज़रूरत है। लेकिन जब वह इस ‘दोहराव’ को व्याख्यायित करते हैं तो उसमें कुछ भी लेनिनवादी नहीं होता बल्कि वे लेनिनवाद की मूल प्रस्थापनाओं को ख़ारिज करते चलते हैं। उदाहरण के लिए, 2009 में ‘आइडिया ऑफ़ कम्युनिज़्म’ नाम से आयोजित एक सम्मेलन में (इसकी चर्चा हम पहले कर चुके है) प्रस्तुत किये गये अपने वक़्तव्य ‘हाउ टू बिगिन फ़्रॉम दि बिगिनिंग’ में लेनिन को दोहराये जाने की बात करते है और इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि आज बीसवीं सदी के समाजवादी प्रयोगों के अध्याय को पूरी तरह से बन्द किये जाने की आवश्यकता है और इसलिए हमें एक ”नयी शुरुआत” करनी होगी। हम देख सकते हैं कि माओ के विचारों का जैसा हस्तगतीकरण और विकृतीकरण बेदियू अपने चिन्तन में करते है, ठीक वही काम स्लावोय ज़िज़ेक लेनिन के सन्दर्भ में करते हैं। ज़िज़ेक जैसे उत्तर-मार्क्सवादी सिद्धान्तकारों के लिए ‘लेनिनवाद’ जैसी अवधारणाएँ महज़ एक ‘कैचवर्ड’ हैं और अपने लेखन में वह जहाँ-तहाँ इसका इस्तेमाल करते चलते हैं।
अब ज़रा देखते हैं कि मार्क्सवाद से अधिक रैडिकल सिद्धान्त देने के चक्कर में ज़िज़ेक किस तरह की सैद्धान्तिक कलाबािज़याँ दिखाते हैं। मसलन, वह दावा करते हैं कि मार्क्स का ‘राजनीतिक अर्थशास्त्र की समालोचना में योगदान’ का वह प्रसिद्ध कथन, जिसमें वे उत्पादक सम्बन्धों और उत्पादक शक्तियों व आर्थिक आधार और अधिरचना के अन्तर्सम्बन्धों के बारे में बताते हैं, वास्तव में इतिहासवाद और उद्भववाद का शिकार है। मार्क्स के इस उद्धरण को अगर आप स्वयं पढ़ें तो उसमें मार्क्स कहीं भी कोई इतिहासवादी या नियतत्ववादी बात नहीं कह रहे हैं। जो वह कह रहे हैं वह सिर्फ़ इतना है : समाज में लोग प्रभावी उत्पादन व्यवस्था के अन्तर्गत अपनी इच्छा से स्वतन्त्र निश्चित उत्पादन सम्बन्धों में बँधते हैं; एक दौर तक प्रभावी उत्पादन सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों के विकास को गति देते हैं, लेकिन इतिहास की एक निश्चित मंज़िल पर उत्पादक शक्तियों का विकास मौजूदा उत्पादन सम्बन्धों के तहत सम्भव नहीं रह जाता; यहाँ से सामाजिक क्रान्ति का युग शुरू होता है (इसका यह अर्थ नहीं है, कि किसी पूर्वनिर्धारित मौके पर इस युग में क्रान्ति का सम्पन्न हो जाना तय है); आगे मार्क्स बताते हैं कि कोई भी व्यवस्था उत्पादक शक्तियों के विकास के मौजूदा ढाँचे के भीतर बाधित होने से पहले नष्ट नहीं हो सकती और नये उत्पादन सम्बन्धों की स्थापना तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि उसके लिए आवश्यक शर्तें मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही पूरी न हो गयी हों (इसका यह अर्थ नहीं है कि वे उत्पादन सम्बन्ध ही पुरानी व्यवस्था के गर्भ में पूर्णतः पैदा हो चुके हों, यहाँ मार्क्स सिर्फ़ अनिवार्य पूर्वशर्तों की बात कर रहे हैं); और अन्त में मार्क्स इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि मानवता अपने लिए वही लक्ष्य निर्धरित कर सकती है, जो लक्ष्य वह वास्तव में प्राप्त कर सकती है। इसका सिर्फ़ इतना ही अर्थ है कि दास समाज या सामन्ती समाज के उत्पीड़ित वर्ग साम्यवादी समाज का सपना नहीं देख सके थे। लेकिन ज़िज़ेक के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। एक सच्चे प्रत्ययवादी-हेगेलवादी के समान वह कहते हैं कि आज के दौर में भी भावी बेहतर समाज के बारे में कोई परिकल्पना नहीं निर्मित की जानी चाहिए। उसे पूरी तरह से गोपनीयता के राज्य की वस्तु माना जाना चाहिए, जिसे ज़िज़ेक ‘कम्युनिज़्म एब्सकॉण्डिटस’ का नाम देते हैं। इसका अर्थ है कि एक ऐसा कम्युनिज़्म जिसके बार में पहले से कोई नक्शा तैयार नहीं किया जाना चाहिए। ज़िज़ेक यहाँ पर एलेन बेदियू के पदचिन्हों पर ही चल रहे हैं। फ़र्क़ इस इतना है कि ज़िज़ेक कहीं सीधे-सीधे यह नहीं कहते कि मार्क्सवाद, पार्टी और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की सोच पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है। लेकिन वास्तव में वह जो करते हैं वह और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। बेदियू अपने इरादों में स्पष्ट हैं और उनकी आलोचना अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान है। लेकिन ज़िज़ेक अपनी सभी बातों को स्वयं ही काटते चलते हैं।
एक अन्य जगह पर ज़िज़ेक कहते हैं कि मार्क्स ने राजनीतिक अर्थशास्त्र की जो आलोचना की है, उसे आज दुहराने की ज़रूरत है, लेकिन कम्युनिज़्म की उस यूटोपियाई समझदारी के बग़ैर जो कि मार्क्स ने प्रस्तुत की। ज़िज़ेक मार्क्स द्वारा राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना को न समझ पाने के कारण ही ऐसा समझते हैं कि मार्क्स की कम्युनिज़्म की समझदारी यूटोपियाई और फ़न्तासी के समान थी। कम्युनिज़्म की मार्क्सवादी परियोजना कोई पूर्वकल्पित या पूर्वनिर्धरित यूटोपिया या फ़न्तासी नहीं थी, बल्कि पूँजीवाद की वैज्ञानिक आलोचना का ही नतीजा थी। जैसा कि मार्क्स कहते थे, ‘कम्युनिज़्म कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे हासिल किया जाना है। यह इतिहास की वास्तविक गति है।’ लेकिन ज़िज़ेक के लिए इतिहास की ऐसी कोई गति नहीं होती। मार्क्स स्वयं कम्युनिस्ट समाज के एक-एक विवरण को पहले से निर्धारित करने के ख़िलाफ़ थे, और ऐसी किसी भी कवायद को वह अनुत्पादक मानते थे। लेकिन ज़िज़ेक कम्युनिस्ट समाज के विषय में मार्क्स के कुछ भी कहने को ग़ैर-मुनासिब मानते हैं!
ज़िज़ेक कहते हैं कि मार्क्स का इतिहासवादी स्कीमा रद्द करने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें आज के पूँजीवाद की तीन चारित्रिक आभिलाक्षणिकताओं पर नज़र डालने की ज़रूरत है। ज़िज़ेक के मुताबिक़ पहली सबसे प्रमुख अभिलाक्षणिकता आज की पूँजीवादी व्यवस्था में मुनाफ़े से लगान (रेण्ट) की ओर संक्रमण या तब्दीली है। ज़िज़ेक यहाँ दो अर्थों में लगान की बात कर रहे हैं – साझा बौद्धिक सम्पत्ति और प्राकृतिक संसाधनों पर एकाधिकर से मिलने वाला लगान। लेकिन इस परिघटना में नया क्या है और इसकी खोज करने का दावा ज़िज़ेक क्यों कर रहे हैं, यह समझ से परे है। वास्तव में इन दोनों परिघटनाओं को मार्क्स और लेनिन दोनों ने ही अपनी रचनाओं में दर्ज किया है। वास्तव में, यह रिकार्डो का सिद्धान्त था कि लगान सम्पत्ति के एकाधिकार से नहीं बल्कि उत्पादन की अलग-अलग स्थितियों से पैदा होता है। जबकि मार्क्स और लेनिन का स्पष्ट रूप में यह मानना था कि लगान सम्पत्ति के एकाधिकार से पैदा होता है और वह अधिशेष का एक हिस्सा बनता है। इस रूप में मुनाफ़े से लगान की ओर जाने की बात करना दरअसल ज़िज़ेक के एक विभ्रम को दिखलाता है और साथ ही यह भी दिखलाता है कि सभी हेगेलीय लकानियन उत्तर-मार्क्सवादियों की तरह ही ज़िज़ेक की समझ भी राजनीतिक अर्थशास्त्र में दयनीय है।
ज़िज़ेक का दावा है कि मार्क्स ने सामान्य बुद्धि (जनरल इण्टेलेक्ट) के निजीकरण की कल्पना नहीं की थी। ज़िज़ेक का यह दावा भी ग़लत है कि मार्क्स ने कभी नहीं सोचा था कि सामान्य बुद्धि का इस पैमाने पर निजीकरण होगा। मार्क्स स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हर प्रकार के श्रम के सभी उत्पाद सामाजिक सम्पत्ति हैं और ज्ञान भी एक सामाजिक सम्पत्ति है। लेकिन पूँजीवाद श्रम के भौतिक उत्पादों और बौद्धिक उत्पादों दोनों का ही निजीकरण करता है। प्राक्-पूँजीवादी युग में सामान्य बुद्धि के विकास का जो स्तर था, उसमें ज़ाहिरा तौर पर बौद्धिक उत्पादों के निजीकरण की प्रवृत्ति कम ही होगी। जैसे-जैसे पूँजीवाद उत्पादन पद्धति आगे बढ़ी, उत्पादक शक्तियों का विकास हुआ, उत्पादकों की राजनीतिक और तकनोलॉजिकल चेतना का स्तरोन्नयन हुआ, वैसे-वैसे उत्पादन में सूचना और तकनीकी पद्धति के ज्ञान का महत्व बढ़ता गया। पूँजीपतियों के बीच की प्रतिस्पर्द्धा और मज़दूर वर्ग की स्वायत्त चेतना (जो बुर्जुआ वर्चस्व से सापेक्षिक रूप से मुक्त हो) के उदय के डर ने बौद्धिक सम्पदा के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। जहाँ तक बौद्धिक सम्पदा के नयेपन और सूचना के सर्वशक्तिशाली बन जाने का प्रश्न है, तो यह मूर्खतापूर्ण दावा है। एक कुल्हाड़ी या चक्का बनाने में भी प्राचीनकाल में सूचना की आवश्यकता होती थी। यह सच है कि सामान्य बुद्धि के स्तरोन्नयन के साथ सूचना की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गयी है, लेकिन उसका निजीकरण और उसका मालकरण कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर उत्तर-मार्क्सवादी चिन्तक इतना विस्मित हों। आलेख के अगले भाग में हम देखेंगे कि नेग्री और हार्ट भी इस परिघटना को लेकर काफ़ी चकित हैं।
उत्तर-मार्क्सवादियों के इस नये सैद्धान्तिकीकरण की मूल बात यह है कि सर्वहारा वर्ग इनके लिए अनुपस्थित हो चुका है और टटपुँजिया वर्ग परिवर्तन का नया अगुआ है। ज़िज़ेक भी एक प्रकार से इसी थीम का अनुसरण करते हैं। शारीरिक श्रम करने वालों का उदाहरण देने की ज़रूरत होती है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा ‘फ़्लाइट अटेण्डेण्ट’ का उदाहरण दे पाते हैं! औद्योगिक सर्वहारा वर्ग का कहीं ज़िक्र भी नहीं होता। अभौतिक उत्पादन (जैसे सूचना का उत्पादन) एक उन्नत दुनिया का प्रतीक है; इसमें कोई शक़ नहीं। यह बात अलग है कि पूँजीवादी व्यवस्था में भौतिक उत्पादन निकृष्ट बन गया है, और अभौतिक उत्पादन उस पर अपना वर्चस्व और प्रभुत्व स्थापित करके बैठा हुआ है। लेकिन पूँजीवाद में सीधा क्या है? संक्षेप में कहें, तो ज़िज़ेक और उनके जैसे तमाम उत्तर-मार्क्सवादियों ने सूचना पूँजीवाद के उदय के साथ आने वाले परिवर्तनों की जो समझदारी प्रस्तुत की है, वह वास्तव में मार्क्सवाद की बुनियादी श्रेणियों को रद्द करने के लिए की गयी है। इसमें तार्किक निरन्तरता की भारी कमी है, और थोड़ी ही पड़ताल पर उसका उथलापन और ओछापन सामने आ जाता है।
अब आते हैं एक नये क़िस्म की बुर्जुआज़ी के उदय बारे में ज़िज़ेक के दावे। पर। जिसे वह उत्तर-आधुनिक पूँजीवाद की दूसरी चारित्रिक अभिलाक्षणिकता मानते हैं। नयी बुर्जुआज़ी की अवधारणा को वह एक लकानियन विचारक ज्याँ क्लॉड मिल्नर से उधर लेते हैं, और उसे अपने विचारधारात्मक खाँचे में फिट करते हैं। इस बुर्जुआज़ी में न सिर्फ़ डॉक्टर, इंजीनियर, आदि जैसे पेशे के लोग भी शामिल हैं, बल्कि इस वर्ग के सम्भावित उम्मीदवारों में ज़िज़ेक विश्वविद्यालय छात्रों को भी गिनाते हैं। ज़िज़ेक का यह दावा है कि इस नयी बुर्जुआज़ी के ऊपरी हिस्से नियमित स्थायी रोज़गार, बेहद ऊँचे वेतनों और विशेषाधिकरों के स्वामी हैं। जबकि निचले हिस्से वे हैं जिनके सिर पर पूँजीवाद ने अनिश्चितता की तलवार लटका रखी है। ये निचले हिस्से ही हैं, जो कि 2011 में वे ”ख़तरनाक सपने” देख रहे थे (‘ऑक्युपाई’ आन्दोलन) जिनकी बात ज़िज़ेक अपनी नयी पुस्तक में करते हैं। ज़िज़ेक मानते हैं कि अरब जनउभार, ब्रिटिश छात्र-युवा आन्दोलन और निम्न वर्गों के दंगे, स्पेन और यूनान में चल रहे आन्दोलन और साथ ही ‘ऑक्युपाई’ आन्दोलन इन्हीं वर्गों की आकांक्षाओं की नुमाइन्दगी करते हैं। ज़िज़ेक इन आन्दोलनों को ”वामपन्थी” अर्थों में क्रान्तिकारी नहीं मानते। उनका कहना है कि इन आन्दोलनों के पास कोई भविष्य दृष्टि नहीं है। लेकिन अगले ही पल ज़िज़ेक को इन आन्दोलनों में ”भविष्य के चिन्ह” भी दिखलायी देते हैं। ऐसे विरोधभासों से ज़िज़ेक का पूरा लेखन कर्म भरा पड़ा है।
बेदियू की ही तरह इतिहास के प्रति अवहेलना का दृष्टिकोण ज़िज़ेक का भी है, लेकिन अपनी क़िस्म से। वह इतिहास को पूरी तरह प्रतीकात्मक तो नहीं मानते लेकिन वह बीसवीं सदी में मज़दूर वर्ग द्वारा किये गये समाजवाद के प्रयोगों को बिना किसी विश्लेषण के एक त्रासदी मानते हैं, और इस रूप में उसे लक्षण के रूप में ही देखते हैं, जैसा कि बेदियू कहते हैं। ज़िज़ेक के लिए भी बीसवीं सदी के समाजवाद की तरफ़ एक भी दृष्टि डाले हुए भी भावी कम्युनिस्ट समाज का निर्माण हो सकता है। ज़िज़ेक ने अपनी किसी भी रचना में बीसवीं सदी के समाजवाद को, विशेषकर रूस और चीन में समाजवादी प्रयोगों के अनुभवों को एक बुरे अनुभव, त्रासदी या विपदा के तौर पर चित्रित करने के लिए किसी वैज्ञानिक-ऐतिहासिक विश्लेषण का इस्तेमाल नहीं किया है। ज़िज़ेक के लेखन में यह नतीजा आकाशवाणी के समान (axiomatic) है। वह तो यहाँ तक कहते हैं कि आज के समय में कम्युनिस्ट तब तक नया कुछ नहीं कर सकते, जब तक कि वह बीसवीं सदी के समाजवादी प्रयोगों की तरफ़ देखना पूरी तरह से बन्द नहीं कर देते और यह मान नहीं लेते कि वे पूर्ण असफलता में समाप्त हुए। इस इतिहास-दृष्टि के बारे में जितना कम कहा जाये, उतना बेहतर है।
पूँजीवाद-विरोधी प्रतिरोध आन्दोलनों की समीक्षा करते हुए कहते है कि आज जो पूँजीवाद-विरोधी प्रतिरोध आन्दोलन हो रहे हैं वह बेहद अराजकतापूर्ण हैं और अस्त-व्यस्त (messy) हैं। लेकिन उन्हें इसी रूप में स्वीकार करने की ज़रूरत है। अस्त-व्यस्त आन्दोलनों के सैद्धान्तिकीकरण के व्यवस्थित होने की ज़िज़ेक विरोध करते हैं। अगर वस्तुगत परिस्थिति में अराजकता, उथल-पुथल और अस्त-व्यस्तता है, तो इसका यह नतीजा कैसे निकाला जा सकता है उसका सैद्धान्तिक विश्लेषण भी अस्त-व्यस्त होना चाहिए? एक तरफ़ तो ज़िज़ेक मौजूदा प्रतिरोध-आन्दोलनों को ज्यों का त्यों स्वीकार करने की हिमायत करते हैं, वहीं दूसरी ओर वह उनकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि वे मौजूदा व्यवस्था का अंग हैं, और चूँकि उनके पास किसी भावी कम्युनिस्ट समाज का प्रस्ताव या विज़न नहीं है, इसलिए वे प्रगतिशील नहीं हैं, बल्कि वे उन वर्गों के आन्दोलन हैं जिन्हें अपनी विशेषाधिकर-प्राप्त सामाजिक स्थित के खोने का भय है। इसके बाद वह यह भी कहते हैं कि भावी कम्युनिज़्म के बारे में कोई विज़न या ठोस प्रस्ताव होना ही नहीं चाहिए, और हमारा प्रस्ताव होना चाहिए कम्युनिज़्म एब्सकॉण्डिटस! अब आप ही बतायें कि ज़िज़ेक आख़िर कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं! यह सारा सैद्धान्तिक तमाशा एक निष्क्रिय उग्रपरिवर्तनवाद के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे लकानियन शोरबे और हेगेलीय मसाले के साथ छद्म-मार्क्सवादी अँगीठी पर परोसा जा रहा है। इसका कोई ऑपरेटिव पार्ट नहीं है।
हम देख सकते हैं कि छद्म-मार्क्सवादी आवरण में ज़िज़ेक मार्क्सवाद की स्थापित बुनियादी प्रस्थापनाओं को ख़ारिज करने की ही कोशिश करते है। भावी मुक्तिकामी परियोजना की कोई तस्वीर न तो वह पेश करते हैं न ही ऐसा करने के हिमायती हैं। वह अगर कुछ करने में सक्षम हैं तो वह है निष्क्रिय उग्रपरिवर्तनवादी और नुक़सानदेह रूप से भ्रामक सैद्धान्तिकीकरण, जिसके ज़रिये वह दुनिया की एक बेहद दयनीय रूप से असफल व्याख्या ही कर पाते हैं।
‘ऑपराइज़्मो’ (मज़दूरवाद) की ज़मीन पर एण्टोनियो नेग्री-माइकल हार्ट की ‘अमूर्त’ ‘अभौतिक’, ‘आकारविहीन’ सैद्धान्तिकी
दार्शनिकों ने
दुनिया की तरह-तरह से व्याख्या की है
पर सवाल उसको बदलने का है।
लेकिन हम ख़ुद सोचेंगे
सभी सवालों पर फिर से,
नये ढंग से।
हर पुरानी चीज़ पर
सवाल उठाना हैं हमें
जैसे कि इस कथन पर भी
कि दार्शनिकों ने …
– कात्यायनी (दुनिया बदलने के बारे में कतिपय सुधीजनों के विविध विचार-6)
अपनी बहुचर्चित पुस्तक ‘एम्पायर’ (2000) के फ़्रांसीसी संस्करण की शुरुआत एण्टोनियो नेग्री और माइकल हार्ट इस दावे के साथ करते हैं कि इस पुस्तक के ज़रिये उन्होंने ”इक्कीसवीं सदी का नया कम्युनिस्ट घोषणापत्र” लिखने की कोशिश की है। इसके अलावा नेग्री और हार्ट का यह भी मानना है कि जहाँ अन्य उत्तर-मार्क्सवादी विचारक पुरानी शब्दावली से ही काम चला रहे हैं, वहाँ इन दोनों ने नयी शब्दावली गढ़ी है। वैसे इस नयी शब्दावली के पीछे की पूरी सैद्धान्तिकी में मार्क्सवाद को छोड़कर सब कुछ मिल जाता हैं। इसमें आपको स्पिनोज़ा का प्रकृतिवादी यान्त्रिक भौतिकवाद मिल जायेेगा; गिलेश डेल्यूश, फ़ेलिक्स ग्वातारी, मिशेल फ़ूको का उत्तर-आधुनिकतावाद मिल जायेेगा; यहाँ तक कि अमेरिकी संघवादी जेम्स मैडिसन का सिद्धान्त भी आपको इनके लेखन में मिल जायेेगा, साथ ही नेग्री-हार्ट की इस अजीबो-ग़रीब मिश्रण वाली उत्तर-मार्क्सवादी सैद्धान्तिकी की जड़ में इतालवी मज़दूरवाद (ऑपराइज़्मो) की ग़ैर-मार्क्सवादी अर्थवादी सोच है। नेग्री-हार्ट की प्रातिनिधिक रचनाओं – ‘एम्पायर’ (Empire, 2000), मल्टीट्यूड (Multitude, 2004), कॉमनवेल्थ (Commonwealth, 2009) के सन्दर्भ में संक्षिप्त चर्चा करते हुए हम इनके प्रमुख राजनीतिक-विचारधारात्मक सैद्धान्तिकीकरणों की पड़ताल करेंगे। चूँकि मज़दूरवाद का इतालवी संस्करण (ऑपराइज़्मो) लेखकद्वय की सैद्धान्तिकी में एक विशेष स्थान रखता है, बल्कि यूँ कहें तो इनकी पूरी उत्तर-मार्क्सवादी सैद्धान्तिक अट्टालिका, मज़दूरवाद के राजनीतिक आधार पर खड़ी है, इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि एक सरसरी निगाह हम ऑपराइज़्मो की इस विशिष्ट इतालवी परिघटना पर भी डालें।
अंटोनियो (टोनी) नेग्री ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इटली में 1950-1960 के दशक के मज़दूर आन्दोलनों में शिरकत से की। 1970 के दशक के ऑटोनोमिस्ट आन्दोलन के प्रमुख नेता और सिद्धान्तकारों में से एक रहे नेग्री रोमन कैथोलिक ग्रुप (GIAC) से भी जुड़े हुए थे। 1956 से 1963 तक इतालवी समाजवादी पार्टी के सदस्य भी रहे। पार्टी छोड़ने के बाद इतालवी ऑपराइज़्मो के जन्मदाता मारियो ट्रोण्टी के साथ जुड़े। 1950 के दशक की शुरुआत में मारियो ट्रोण्टी इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी (PCI) के सदस्य थे। पार्टी छोड़ने के बाद 1959 में वह इतालवी समाजवादी रैनिएरो पांशिएरी के साथ Quadoni Rossi (Red notebook) नामक पत्रिका निकालने लगे। 1966 में उन्होंने Operai e Capitale (Workers and Capital) लिखा और 1967 में पार्टी में फिर लौट आये ताकि ऑपराइज़्मो को एक सिद्धान्त के तौर पर पार्टी के अन्दर भी लागू किया जा सके।
1968 में ओपराइस्टों (मज़दूरवादियों) के समूह में मुख्य रूप से दो मुद्दों पर फूट पड़ गयी। पहला मुद्दा था, इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों का प्रभुत्व और दूसरा मुद्दा था, CGIL (General Italian Confederation of Workers) द्वारा सामाजिक संघर्षों में हस्तक्षेप एवं मध्यस्थता की पद्धति पर ज़्यादा ज़ोर देने की आवश्यकता को रेखांकित किया जाना। नेग्री ने 1968 में ट्रोण्टी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि नेग्री का मानना था कि पी.सी.आई. की राजनीति अब कोई नया मोड़ नहीं ले सकती है, जबकि ट्रोण्टी एक और कोशिश करने की बात कह रहे थे। इसी समय नेग्री ने पोतेरे ओपराइया नामक ग्रुप की स्थापना की जो 1968 से 1973 तक सक्रिय रहा और 1975 में ऑटोनोमिया आन्दोलन से जुड़ गया।
इतालवी मज़दूर आन्दोलन में ऑपराइज़्मो की धारा 1960 के दशक में जड़ जमाने लगी। चूँकि कोई क्रान्तिकारी विकल्प मौजूद नहीं था (इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी का संशोधनवादी और समझौता-परस्त चरित्र 1950-60 का दशक आते-आते साफ़ हो चुका था) इसलिए ऑपराइज़्मो जैसी विजातीय प्रवृत्तियों को मज़दूर आन्दोलन के बीच फलने-फूलने का मौक़ा मिला। ऑपराइज़्मो धारा के मुख्य सिद्धान्तकार थे – मारियो ट्राण्टी, एण्टोनियो नेग्री और पाउलो विरनो। 1960 एवं 1970 के दशक इटली की जनता में फैले भयानक असंतोष और जनउभारों के दशक हैं। तत्कालीन सरकार की आर्थिक नीतियों ने कृषि आधारित दक्षिणी इटली से औद्योगिक क्षेत्र उत्तरी इटली की ओर प्रवास की स्थिति पैदा कर दी। औद्योगिक क्षेत्र को सस्ता श्रम मिल रहा था लेकिन सरकार इतनी बड़ी जनसंख्या को शहरों में गुज़र करने के लिए अन्य सुविधएँ देने में असमर्थ थी। इस स्थिति ने मज़दूर आन्दोलनों को जन्म दिया। ये मज़दूर आन्दोलन जल्दी ही जनता के आन्दोलनों में तब्दील हो गये। 1962 में तूरिन में फियेट (Fiat) के मज़दूरों ने बड़ी हड़ताल की। 1968 में बड़े पैमाने पर हड़तालें और हिंसात्मक घटनाएँ हुईं। इसी दौरान 1970 में विश्व पूँजीवाद मन्दी के दौर में प्रवेश कर चुका था और दुनिया भर में (फ़्रांस, जर्मनी, ग्रीस आदि) जनता के आन्दोलनों का दौर शुरू हो चुका था। 1975 में इटली में ऑटोनोमिया आन्दोलन शुरू हुआ जिसमें बड़ी संख्या में मज़दूर, स्त्रियाँ, छात्रा, युवा बेरोशगार सभी शामिल थे। यह आन्दोलन स्वतःस्फूर्त और प्रतिनिधित्व-विरोधी (anti-representation) था। ओपेराइस्ट (Operaist) विचारकों ने इन आन्दोलनों से अपनी सैद्धान्तिक प्रामाणिकता प्राप्त की। इनमें लिबरटैरियन, अराजकतावादी, नव-अराजकतावादी, ”विचारधारा-मुक्त” राजनीतिक कार्यक्रम यानी कि मज़दूर आन्दोलनों की हर क़िस्म की विजातीय प्रवृत्तियाँ मौजूद थीं।
मज़दूरवाद का इतालवी संस्करण ऑपराइज़्मो ”मज़दूर वर्ग की संरचना” में आये ”बदलावों” को रेखांकित करने की बात करता है। तात्पर्य यह है कि वह सर्वहारा वर्ग को नये तरीके से परिभाषित करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार, दिहाड़ी मज़दूर (wage earning workers), कर्मचारी (white coller), शारीरिक श्रम करने वाले औद्योगिक मज़दूर (blue collar) और छात्र, बेरोज़गार युवा, घरेलू कामगार आदि सभी इस ”नये सर्वहारा” में शामिल हैं। इनमें वे सभी हैं जो यूनियन के किसी भी रूप में संगठित नहीं हैं। यह सिद्धान्त ”मास वर्कर्स” के ”सोशलाइज़्ड वर्कर्स” में रूपान्तरण की अवधारणा देता है। यह सोशलाइज़्ड वर्कर उच्च शिक्षा प्राप्त, बौद्धिक कार्यों के ‘मानकीकरण’ एवं ‘सर्वहाराकरण’ से पैदा हुआ वर्ग था। यह वर्ग अकुशल एवं शारीरिक श्रम करने वाले ”मास वर्कर” से भिन्न था। नेग्री-हार्ट की ‘अभौतिक श्रम’ (immaterial labour) की अवधारणा का स्रोत सर्वहारा वर्ग की यही ‘नयी परिभाषा’ है। ऑपराइज़्मो राज्य, ट्रेड यूनियन, पार्टी या किसी भी तरह के अनुशासित राजनीतिक संगठन से मज़दूर वर्ग को मुक्त रखने का हिमायती है तथा ”स्वतः संगठित प्रतिरोध” को प्रधनता देता है, क्रान्ति की जगह ”विप्लव” की बात करता है लेकिन ”विप्लव” कब, कौन, कैसे करेगा; इसका कोई जवाब नहीं देता –
”हम क्रान्ति नहीं विप्लव की बात करते हैं : आज यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पूँजी द्वारा सर्वहारा के एकजुट मोर्चे को तोड़ने के लिए ली गयी पूर्ण पहलक़दमी को लगातार परास्त किया जायेे।” (Crisi dello stato-Piano, Negri, pg. 42)
आगे नेग्री ने लिखा है, कि लेनिन ने सर्वहारा के एकीकरण की जो प्रक्रिया बतायी है वह आधुनिक विश्व में उलट गयी है। अब पार्टी के नेतृत्व में ”ऊपर से नीचे” (Top-down process) की प्रक्रिया की जगह ”जन अग्रगामी समूह” (mass avant gardes) से उत्प्रेरित ”नीचे से ऊपर” (bottom-up) प्रक्रिया की ज़रूरत है। यह लेनिनवादी पार्टी और हिरावल की अवधारणा को ख़ारिज करना ही है। ऑपराइज़्मो ने एक और विचित्र क़िस्म का सैद्धान्तिकीकरण पेश किया है। इसे अस्वीकरण के सिद्धान्त (Theory of refusal) की संज्ञा दी गयी। इसके अनुसार मज़दूर वर्ग, पूँजीवादी व्यवस्था को अपना श्रम देने से इंकार और पूँजीवादी विकास में अपनी सहभागिता से इंकार करेगा। यह कैसे सम्भव होगा, ऑपराइज़्मो के सिद्धान्तकार यह बताना ज़रूरी नहीं समझते। ऑपराइज़्मो के संक्षिप्त परिचय के बाद हम नेग्री और हार्ट के सैद्धान्तिक लेखन पर बात करेंगे।
नेग्री और हार्ट की सैद्धान्तिकी पर विस्तार से बात करने से पहले सारतः कुछ बातें स्पष्ट कर देनी ज़रूरी हैं। पहली, यह कि नेग्री और हार्ट के अनुसार मार्क्सवादी सिद्धान्त एवं पद्धति पिछले 150 वर्षों, विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पैदा हुए नये यथार्थ को समझने के लिए नाकाफ़ी है। मार्क्सवाद को सिरे से ख़ारिज करते हुए लेखकद्वय का विचार है कि आज आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को एक नया रूप चुनना होगा। ऐसी नयी अवधारणाएँ खोज निकालनी होंगी जो नये यथार्थ के अनुरूप हो और बड़े पैमाने पर जनता के राजनीतिक संघर्ष की वस्तुगतता की पुनर्स्थापना करे। (यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि वह रूप कैसा होगा?) दूसरी, कि जिस प्रकार पूँजीवाद के अन्दर समाजवाद के भौतिक आधार मौजूद होते हैं उसी तरह आज इस भूमण्डलीकरण ने सामाजिक एवं आर्थिक न्याय पर आधारित एक विश्वव्यापी समाज की ज़मीन तैयार कर दी है। उत्पादन एवं श्रमिक वर्ग की संरचना में आये बदलावों ने पूँजी के उत्पीड़न और दमन के खिलाफ़ संघर्ष के नये अवसर पैदा किये हैं। ऐसे सिद्धान्त-प्रतिपादनों के द्वारा नेग्री-हार्ट पूँजीवाद साम्राज्यवाद के ‘अपॉलोजिस्ट्स’ की भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। तीसरी, कि आज साम्राज्यवाद का दौर नहीं ”एम्पायर” (Empire) का दौर है इसलिए देशीय या क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष का कोई मतलब नहीं है और सर्वहारा वर्ग जैसा कोई केन्द्रीकृत वर्ग नहीं है, बल्कि निर्गुण, निराकार ”मल्टीट्यूड” है जो किसी राज्य-सत्ता के अन्तर्गत नहीं बल्कि ”ग्लोबल सिटीज़नशिप” के अन्तर्गत है और विप्रादेशिकृत (deterritorialized) है। चौथी, कि यह ”मल्टीट्यूड” सामाजिक स्तर पर उत्पीड़ित ”भूमण्डलीकृत जनसंख्या” है जो ”एम्पायर” के अन्दर ही गठित हो रही है। यह मल्टीट्यूड ‘एम्पायर’ के खिलाफ़ परस्पर सहभागिता और सहकार के आधार पर साझा सम्पदा ”कॉमन” (Common) की खोज करेगा और स्वतः ही संगठित होगा। यह बात दीगर है कि उनकी किताब ‘कॉमनवेल्थ’ के दो सौ पन्ने इसी बात की असफल खोज करते हुए रंगे गये हैं कि यह ”कॉमन’ अस्तित्वमान कैसे होगा! पाँचवीं, कि बीसवीं शताब्दी के तमाम क्रान्तिकारी प्रयोग ग़ैर-जनवादी और निरंकुश शासन (Tyranny) थे इसलिए ”कॉमन” की खोज करनी होगी।
अब नेग्री-हार्ट की सैद्धान्तिकी के विस्तार पर आते हैं। अपने लेखन में नेग्री और हार्ट पूँजीवाद या साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग नहीं करते बल्कि ‘एम्पायर’ की बात करते हैं। यह ‘एम्पायर’ किसी भी सीमा में नहीं बँधा हुआ है और इसका कोई केन्द्र नहीं है। यह कोई ऐतिहासिक सत्ता नहीं बल्कि निरपेक्ष सत्ता है। यहाँ नेग्री-हार्ट, डेल्यूज़ और ग्वातारी जैसे उत्तर-आधुनिकतावादियों से ”डिटेरिटोरिअलाइज़ेशन” की अवधारणा ले आते हैं जिससे उनका तात्पर्य है पूँजी और जनसंख्या का सीमातीत ग्लोबल प्रसार। उनके अनुसार यह ‘एम्पायर’ इतिहास की गति में कोई अवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसी सत्ता है जो इतिहास से बाहर है या इतिहास के अन्त पर है। यह मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को ही संचालित नहीं करता है बल्कि मानव प्रकृति को भी शासित करता है और समाज में गहरायी तक व्याप्त है। इस प्रकार यह ‘बायोपॉवर’ (जैवशक्ति) का पैराडाइम रचता है। ‘बायोपॉवर’ की यह अवधारणा फ़ूको की दी हुई है जिसके अनुसार ‘बायोपॉवर’ आधुनिक राष्ट्र-राज्य (Nation State) और पूँजीवाद द्वारा ”बॉडीज़” (Bodies) को अधीन करके जनसंख्या पर नियन्त्रण रखता है। यहाँ फ़ूको व्यक्ति को एक जैविक सत्ता के रूप में ”बॉडी” का नाम देता है। अब आइये इस पूरे बौद्धिक-सैद्धान्तिक गड़बड़झाले की पड़ताल करते हैं।
‘डिटेरिटोरियलाइज़ेशन’ की इस अवधारणा में इसके नाम के अलावा कुछ भी नया नहीं है। विस्तार और प्रसार तो पूँजी की चारित्रिक विशेषता है और नैसर्गिक गति है। बिना स्वयं को प्रसारित किये वह अपना अस्तित्व नहीं बचा सकती। इसलिए भूमण्डलीकरण के दौर में वह अपने वैश्विक प्रसार से सभी बाधओं को हटाते जाती है ताकि वित्तीय पूँजी एवं माल का आगमन-निगमन सुगम बनाया जा सके। इस यथार्थ का सैद्धान्तिकीकरण मार्क्सवाद ने ही किया था। फैशनेबल नाम देकर उत्तर-मार्क्सवादी इसे अपना आविष्कार बताने पर तुले हुए हैं। जहाँ तक मिशेल फ़ूको के ”बायोपावर” और ”बायोपॉलिटिक्स” जैसी अवधारणाओं का प्रश्न है तो यह सत्ता की अपराजेयता को ही रेखांकित करने के लिए गढ़ी गयी हैं। यह उसी पुरानी फू़कोल्डियन उत्तर-आधुनिकतावादी सैद्धान्तिकी का विस्तार मात्रा है कि सत्ता पोर-पोर में समायी हुई है और इसलिए सत्ता का सामूहिक प्रतिरोध व्यर्थ है। इस सिद्धान्त के अनुसार सत्ता का सामूहिक प्रतिरोध हर-हमेशा स्वयं सत्ता की संरचनाओं को जन्म देगा इसलिए इस प्रतिरोध को वैयक्तिक और निजता की जगत में हर प्रकार के सार्वभौमिक और मानक को तोड़ कर किया जाना चाहिए।
बकौल नेग्री-हार्ट ”एम्पायर” के अंदर एक ऐसी प्रतिरोधी ताक़त पैदा हो रही है जो इसे परास्त करेगी। वह ताक़त है ”मल्टीट्यूड”। यह ”मल्टीट्यूड” उनके लिए वर्ग का स्थानापन्न है। इसकी अवधारणा को विकसित करते हुए लेखकद्वय ”श्रम की संरचना” में आये ”बदलावों” की ओर इंगित करते हैं और ”अभौतिक श्रम” (Immaterial labor) की एक नयी अवधारणा देते हैं। उनके अनुसार बीसवीं सदी के अन्तिम दशकों में औद्योगिक श्रम का वर्चस्व ख़त्म हो गया और इसकी जगह ”अभौतिक श्रम” स्थापित हो गया। यह अभौतिक श्रम ज्ञान, सूचना, संचार, रिलेशनशिप, भावनात्मक संप्रेषण आदि उत्पादित करता है। यानी सेवा क्षेत्र, बौद्धिक श्रम और संज्ञानात्मक श्रम ”अभौतिक श्रम” हैं। इस अभौतिक श्रम के द्वारा जो उत्पादन पैदा होता है यह ”बायोपोलिटिकल उत्पादन” है। बायोपोलिटिकल इसलिए कि यह विचार, इमेज, संकेत उत्पादित करता है। यह उत्पादन स्वायत्त है और इसे मापा नहीं जा सकता है। यही बायोपोलिटिकल उत्पादन ‘मल्टीट्यूड’ को परस्पर सहभागिता एवं सहकार की ओर ले जायेेगा।
क्रान्तिकारी वर्ग राजनीति को ख़ारिज करते हुए वे कहते हैं कि, क्रान्तिकारी वर्ग राजनीति का उद्देश्य बस सभी को सार्वभौम रूप से दो वर्गों – बुर्जुआ और सर्वहारा में बाँट देना है और इसलिए सामाजिक समानता पर आधारित संरचना पैदा कर पाने में वह असमर्थ है। आज चूँकि अलग-अलग अस्मिताओं और ”सिंग्युलैरिटी” का सवाल अहम है इसलिए इस तरह की राजनीति अप्रासंगिक है। आज सिर्फ़ ”ग़ैर-क्रान्तिकारी परियोजनाएँ” ही मज़दूरों की अस्मिताओं की रक्षा कर सकती हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि वही पुराना उत्तर आधुनकितावादी राग है जो अस्मितावादी राजनीति की बात करता है। अब चूँकि क्षेत्र, जाति, भाषा, नस्ल, धर्म की विभिन्नताएँ मौजूद हैं इसलिए इन्हें एक ही चीज़ है जो समाहित कर सकती है, वह है परम ”उदार” ”मल्टीट्यूड” जो ”एकता में अनेकता” का मॉडल देता है।
नेग्री व हार्ट आगे बताते है कि अब राजनीतिक संघर्ष ‘निष्क्रमण’ (Exodus) के रूप में होगा। मल्टीट्यूड समय के साथ परिपक्व होगा और इस अवस्था में पहुँचेगा कि ”बायोपोलिटिकल उत्पादन” में पैदा हुए श्रम की स्वायत्तता के बल पर ख़ुद को ”एम्पायर” से अलग कर लेगा। (Commonwealth, पृ. 153) दरअसल इस ”एक्सोडस” की जड़ें ऑपराइज़्मो के ”अस्वीकरण सिद्धान्त” में हैं। लेकिन इतना सारा ”अहम कार्य” मल्टीट्यूड करेगा कैसे? अब श्रीमान नेग्री-हार्ट को तो पार्टी और हिरावल जैसी अवधारणाओं से परहेज़ है, क्योंकि इस तरह के संगठन ”अस्मिता” का हनन कर देते हैं इसलिए सहभागिता, स्वायत्तता और ”नेटवर्क संगठन” (Network Organisation) ही उसे संगठित करेंगे। अब आपको नेग्री और हार्ट बारहवीं शताब्दी में ले जाते हैं और एक ”सोशल वर्कर” की अवधारणा देते हैं। यह सोशल वर्कर 12वीं शताब्दी के इतालवी कैथोलिक उपदेशक सेंट फ़्रांसिस ऑफ़ असीसी का चोगा पहनकर आदर्शवादी रूप में ”ड्यूटी” और ”अनुशासन” से काम करते हुए ”नेटवर्क संगठन” बनायेगा। बकौल नेग्री-हार्ट सेंट फ़्रांसिस ही ”भविष्य की राजनीति को रास्ता दिखायेंगे” (Empire, p. 413)। तो नेगी-हार्ट द्वारा प्रस्तावित मुक्तिकामी राजनीति के मॉडल – एक कैथोलिक धर्म गुरु हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन सट्टेबाज़ दार्शनिकों का धुरीविहीन चिन्तन इन्हें कहाँ ले आया – सीधे धर्म की गोद में!
अब ज़रा बीसवीं शताब्दी के समाजवादी प्रयोगों और समाजवादी संक्रमण पर नेग्री-हार्ट की ”मौलिक” प्रस्थापनाओं पर भी एक सरसरी निगाह दौड़ाई जाये। बकौल नेग्री-हार्ट समाजवादी संक्रमण ”बायोपोलिटिकल इकोनॉमी” को नियन्त्रित करने में अक्षम है। आज उत्पादन औद्योगिक नहीं रहा बायोपालिटिकल (अभौतिक) हो गया है इसलिए समाजवाद की प्रासंगिकता ख़त्म हो गयी है। हालाँकि बीसवीं शताब्दी में एक शक्तिशाली आर्थिक मॉडल दिया गया लेकिन यह समझना आवश्यक है कि समाजवाद और पूँजीवाद कभी भी परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि समाजवाद पूँजीवादी उत्पादन के राज्य द्वारा प्रबन्धन का दौर है। यह चूँकि औद्योगिक पूँजी के प्रोत्साहन और विनियमन के लिए काम करता है इसलिए श्रम के अनुशासन की एक ऐसी सत्ता क़ायम करता है जो सरकार एवं नौकरशहाना संस्थाओं के द्वारा चलायी जाती है (Commonwealth, पृ. 269, 361, 362)। चूँकि समाजवाद औद्योगिक पूँजी के ”पैराडाइम” से निकलता नहीं इसलिए सारी क्रान्तियाँ विफल हो गयीं! वे आगे कहते हैं कि सोवियत यूनियन के अन्तिम दशकों में सामाजिक उत्पादन की आन्तरिक गतिकी और इसके राह की बाधाओं को देखना पड़ेगा। 1960 से 1980 के दशकों में सांस्कृतिक और विचारधारात्मक वातावरण विकसित हो रहा था जिसे समाजवादी व्यवस्था द्वारा दबाने की कोशिश की गयी। चूँकि इस रचनात्मकता की राह में बाधा खड़ी की गयी इसलिए स्थिरता की स्थिति बन गयी और उस दौरान हो रहा बायोपोलिटिकल उत्पादन दबकर रह गया।
तो बीसवीं सदी के समाजवादी प्रयोगों की यह बचकानी आलोचना नेग्री-हार्ट पेश करते हैं! इसे आलोचना कहना भी आलोचना शब्द का मज़ाक उड़ाना होगा! एक तो यह तथ्यात्मक रूप से भी ग़लत है। 1960 से 1980 के दशक जिसे नेग्री-हार्ट समाजवादी काल मान रहे हैं, वह तो समाजवाद का दौर था ही नहीं। दूसरे ”बायोपॉलिटिकल इकॉनमी” यानी की सूचना के उत्पादन (अभौतिक उत्पादन) की सम्भावनासम्पन्नता के प्रति इन विचारकों में एक प्रकार का फ़ेटिश (अन्धभक्ति) है। एक बात जो ये ‘चिन्तक’ नज़रअन्दाज कर जाते हैं वह यह कि उत्पादन में सूचना का कितना भी महत्व हो जायेे (और ऐसा कब नहीं था), भौतिक उत्पादन का महत्व और उसकी मानव जीवन के लिए अनिवार्यता किसी भी सूरत में कम नहीं हो सकती। अभौतिक उत्पादन करने वालों को भोजन, मकान, कपड़े व अन्य भौतिक वस्तुओं की ज़रूरत होगी, और इनके मिलने के बाद ही वह अभौतिक उत्पादन कर सकता है। साथ ही, आज सिर्फ़ संख्यात्मक तौर पर भी देखा जाये तो भौतिक उत्पादन करने वालों की तादाद अभौतिक उत्पादन करने वालों से कहीं ज़्यादा है। लेकिन भौतिक और अभौतिक उत्पादन के बीच इस प्रकार का बँटवारा ही अवैज्ञानिक और अतार्किक है।
इनकी पूरी सैद्धान्तिकी का सार-संक्षेप करे तो नेग्री और हार्ट जिस अभौतिक उत्पादन, अभौतिक श्रम और अभौतिक पूँजीवाद की बात करते है, जिसके अनुसार आज पूँजीवादी विश्व में सूचना प्रमुख और प्रभावी उत्पाद/माल बन चुकी है, और इसके उत्पादन में लगी श्रमशक्ति प्रमुख श्रम शक्ति बन चुकी है, वह इसीलिए गढ़ा गया है कि सर्वहारा वर्ग की परिभाषा को प्रदूषित किया जा सके। एक अभौतिक पूँजीवाद के नाश के लिए वह एक आकृतिविहीन आकारविहीन मल्टीट्यूड की कल्पना करते हैं। यह मल्टीट्यूड एक उतने ही आकारविहीन और आकृतिविहीन क़िस्म के शासकों के समूह (एम्पायर) का तख्तापलट कर, कॉमन्स (साझा-सम्पदा) को निजी कब्ज़े से मुक्त करायेगा। इनकी सैद्धान्तिकी में पूँजीवाद एक अवैयक्तिक (इम्पर्सनल) शक्ति बन जाता है, प्रतिरोध एक अमूर्त चीज़ बन जाती है और प्रतिरोध करने वाले भी आकृतिविहीन वस्तु बन जाते हैं। यह पूरी अवधारणा बुनियादी मार्क्सवादी सिद्धान्तों, जैसे कि वर्ग की अवधारणा, निजी सम्पत्ति और पूँजी की अवधारणा, पार्टी और राज्य की अवधारणा आदि पर हमला करने के लिए ही गढ़ी गयी है।
अर्नेस्टो लाक्लाऊ और चैण्टल माउफ़ की ‘उग्रपरिवर्तनवादी जनवाद’ की अवधारणा : उत्तर-आधुनिकतावादी अस्मितावादी राजनीति की एक और सैद्धान्तिकी
दार्शनिकों ने
दुनिया की तरह-तरह से व्याख्या की है
पर सवाल उसको बदलने का है,
लेकिन मुकम्मिल तौर पर
बदलना इस दुनिया को
मेरे बूते की बात नहीं।
इसलिए मैं पैबन्द लगाता हूँ।
– कात्यायनी (दुनिया को बदलने के बारे में कतिपय सुधीजनों के विविध विचार-4)
आज उत्तर-मार्क्सवादी ‘दार्शनिकों’ की नयी खेप (बेदियू, ज़िज़ेक, नेग्री-हार्ट आदि) के अवतरित होने के साथ अर्नेस्टो लाक्लाऊ और चैण्टल माउफ़ के सैद्धान्तिकीकरण बौद्धिक जगत से थोड़े ‘आउटडेटेड’ हो गये हैं। क्या करें, आजकल इनसे भी ज़्यादा ”रैडिकल” और गर्मागर्म जुमलों का इस्तेमाल करने वाले ”चिन्तकों” के ”चिन्तनों” का बाज़ार गर्म है! लेकिन 1985 जब ‘हेजेमनी एण्ड सोशलिस्ट स्ट्रैटजी : टुवर्ड्स ए रैडिकल डेमोक्रेटिक स्ट्रैटजी : टुवर्ड्स ए रैडिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स’ प्रकाशित हुई थी तब इसे राजनीतिक सिद्धान्त की मार्क्सवादी परम्परा में एक ”ब्रेकथ्रू” रचना के तौर पर देखा जा रहा था क्योंकि यह ”मरणासन्न, जड़, कठमुल्लावादी” मार्क्सवादी सिद्धान्त से उत्तर-संरचनावादी, ”उत्तर-मार्क्सवादी” दर्शन की तरफ़ संक्रमण का संकेत दे रही थी। इस मायने में लाक्लाऊ-माउफ़ को उत्तर-मार्क्सवादी सैद्धान्तिकी के जन्मदाता के तौर पर भी देखा जा सकता है। हालाँकि, आज इनका रचनाकर्म अकादमिक दायरों में उतनी हलचल नहीं पैदा कर पा रहा है, लेकिन आज तक ज़िज़ेक जैसे अधिक फैशनेबल उत्तर-मार्क्सवादी, लाक्लाऊ-माउफ़ की कई अवधारणाओं की बुनियाद पर ही अपने नित-नये सैद्धान्तिकीकरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
लाक्लाऊ और माउफ़, अपनी उक्त पुस्तक में क्रान्तिकारी सम्भावना की हर बात को ख़ारिज करते हुए ”उग्रपरिवर्तनवादी” सुधारवादी परियोजनाओं को हाथ में लेने की हिमायत करते हैं। इनका मानना है कि ‘कठमुल्लावादी’ मार्क्सवाद को उसके ‘सारभूतवादी’ (essentialist) तत्वों (यानी की वर्ग की अवधारणा, क्रान्तिकारी परिवर्तन की अवधारणा, हिरावल के रूप में पार्टी की अवधारणा, सर्वहारा अधिनायकत्व की अवधारणा) से निजात दिलाने के लिए समकालीन उत्तर-आधुनिकतावादी, उत्तर-संरचनावादी दर्शन के सैद्धान्तिक उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही ज़ाक लकाँ, मिशेल फूको, रोलाँ बार्थ, ज़ाक देरिदा जैसे दार्शनिकों से भी काफ़ी कुछ सीखना होगा। मार्क्सवादी सिद्धान्त में अन्तर्निहित ‘आर्थिक नियतत्ववाद’ (economic determinism) को इसी तरह से दुरुस्त किया जा सकता है।
लाक्लाऊ और माउफ़ भी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी विचारकों का अपनी उत्तर-मार्क्सवादी राजनीति के हिसाब से विनियोजन करने में पीछे नहीं रहते। यहाँ इन्होंने अपना निशाना ग्राम्शी को बनाया है। हालाँकि यह सिर्फ़ ग्राम्शी के सिद्धान्तों के हस्तगतीकरण तक नहीं रुकते बल्कि उससे भी आगे जाने की बात करते है! वैसे इसमें भी कुछ नया नहीं हैं! बेदियू माओ से भी आगे निकलकर उत्तर-माओवादी हो गये, ज़िज़ेक लेनिन से भी आगे निकलकर उत्तर-लेनिनवादी हो गये, लाक्लाऊ और माउफ़ ग्राम्शी से आगे निकलकर उत्तर-ग्राम्शीवादी हो गये! और यह सभी मिलकर, मार्क्सवाद की हदों को लाँघकर, मार्क्सवाद से भी अधिक रैडिकल विचारधारा की खोज करते हुए, उत्तर-मार्क्सवादी हो गये हैं!
अपने ‘उग्रपरिवर्तनवादी जनवाद’ की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लाक्लाऊ और माउफ़ कहते हैं कि यह किसी ‘एक राजनीतिक स्पेस’ की बात नहीं करता बल्कि ‘जनवादी संघर्षों’ की ख़ोज ”राजनीतिक ‘स्पेस’ की बहुलता” में यक़ीन करता है। और यहाँ पर लाक्लाऊ और माउफ़ अपनी अस्मितावादी राजनीति की अवधारणा को लाते हैं। वर्ग-आधारित एकजुटता और तदजनित संघर्ष एक क़िस्म की एकाशमीयता और सार्वभौमिकता का निर्माण करते हैं। चूँकि हर क़िस्म की सार्वभौमिकता और सामान्यता दमनकारी होती है इसलिए आज के ‘रैडिकल जनवाद’ की परियोजना को नये सामाजिक आन्दोलनों – जैसे कि पर्यावरण, शान्ति से जुड़े आन्दोलनों, नारीवादी आन्दोलन, समलैंगिकों के आन्दोलन आदि को अपने दायरे में लाना होगा। भारत में कुछ बौद्धिकतावादी मार्क्सवादियों ने लाक्लाऊ और माउफ़ के इस सिद्धान्त को भारत के परिप्रेक्ष्य में जाति, जेण्डर, आदिवासियों आदि के संघर्ष पर लागू किया है और इस थीसिस तक गये हैं कि अब वर्ग संघर्ष अपने क्लासिकीय रूपों में नहीं होगा, बल्कि इन पहचानों के संघर्ष के रूप में होगा; या अब क्लासिकीय वर्ग संघर्ष तमाम ‘जनवादी संघर्षों’ में से एक होगा, जिनमें जाति, जेण्डर आदि के संघर्ष भी शामिल होंगे और वर्ग संघर्ष पर अलग से बल देना नियतत्ववाद होगा। अब तक यह स्पष्ट हो चुका है लाक्लाऊ-माउफ़ का राजनीतिक एजेण्डा वाक़ई में उत्तर-आधुनिकतावादी, अस्मितावादी राजनीति का एजेण्डा ही है। इनके लिए वर्ग-आधारित राजनीति अतीत की बात है। आज इसका दौर बीत चुका है। आज के दौर में सुधारवाद के ज़रिये, पैबन्दसाज़ी के ज़रिये पूँजीवादी व्यवस्था के भीतर ही ‘रैडिकल जनवादी’ स्पेस बनाया जा सकता है, इसलिए इनके अनुसार क्रान्तिकारी परिवर्तन की, सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में क्रान्ति की कोई ज़रूरत नहीं रह गयी है। यही इनके सिद्धान्त की मूल अन्तर्वस्तु है।
अन्त में…
इस पूरी चर्चा के बाद हम स्पष्ट तौर पर यह कह सकते हैं कि उत्तर-मार्क्सवाद के अलग-अलग ‘शेड्स’ के ‘सिद्धान्तकारों’ की भाँति-भाँति की सैद्धान्तिकियों का मक़सद मार्क्सवाद की क्रान्तिकारी अर्न्तवस्तु पर हमला करना है। सही मायनों में कहें, तो उत्तर-आधुनिकतावाद के प्रत्यक्ष हमलों के चुक जाने के बाद उत्तर-आधुनिकतावाद का विरोध करने की नौटंकी करते हुए, इन तमाम सट्टेबाज़ उत्तर-मार्क्सवादी दार्शनिकों के धुरी-विहीन चिन्तन और दार्शनिक ख़ानाबदोशी का वास्तविक निशाना एक बार फिर मार्क्सवाद ही है। इनके शब्द अलग हैं; उत्तर-आधुनिकतावाद जिस बेशर्मी के साथ पूँजीवाद की अन्तिम विजय, कोई विकल्प न होने, पहचान की राजनीति के समर्थन, आदि की बात करता था, अब वैसा करना असम्भव है और किसी के लिए ऐसा करना अपना मज़ाक उड़वाने जैसा होगा। इसलिए इन नये दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष तौर पर पूँजीवाद-विरोध की भाव-भंगिमा अपनायी है और पूँजीवाद की ये लोग एक ”नये क़िस्म की आलोचना” करते हैं। आज के ज़माने में पूँजीवाद के ख़िलाफ़ आम जनता सड़कों पर उतर रही है। यह 1990 का दौर नहीं है जब दुनिया भर में पस्ती और निराशा छायी हुई थी। उस समय उत्तर-आधुनिकतावाद नंगे तौर पर ‘अन्त’ की घोषणाएँ कर सकता था। अब कोई भी विचारधारा जो ऐसा प्रयास करेगी, उसके हश्र का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए पूँजीवादी बौद्धिक तन्त्र ने अपनी सहज गति से नये क़िस्म के ”दार्शनिकों” को पैदा किया है जिसमें से किसी को ‘मोस्ट एण्टरटेनिंग थिंकर’, ‘ग्रेटेस्ट लिविंग थिंकर’ आदि कहा जा रहा है तो किसी को ‘मोस्ट इनोवेटिव थिंकर ऑफ़ जेनरेशन’ और पता नहीं क्या-क्या कहा जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इन नये ”दार्शनिकों” का निशाना भी वही है जो कि 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में उत्तर-आधुनिकतावाद, उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धान्त आदि का था – मार्क्सवाद की क्रान्तिकारी अन्तर्वस्तु। आज इन तमाम उत्तर-मार्क्सवादियों दार्शनिकों की दार्शनिक आवारागर्दी की कठोर आलोचना की ज़रूरत है और इनके विचारों के वास्तविक मार्क्सवाद-विरोधी चरित्र को साफ़ करने की ज़रूरत है। यह समझने की ज़रूरत है कि शब्दों के सारे खेल और बाज़ीगरी के पीछे इनका इरादा और मक़सद क्या है।
दिशा सन्धान – अंक 5 (जनवरी-मार्च 2018) में प्रकाशित